कवि नागार्जुन का जीवन परिचय और रचनाएं || kavii Nagarjun ka jivan Parichay
कवि नागार्जुन जी का जीवन परिचय यहां पर सबसे सरल भाषा में लिखा गया है। यह जीवन परिचय कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कवि नागार्जुन जी के सभी पहलुओं के विषय में चर्चा की गई है, तो इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है।
Table of Contents –
नागार्जुन
(जीवनकाल : सन् 1911-1998 ई०)
जनवादी कवि नागार्जुन का जन्म सन् 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इन्होंने अपनी रचनाएं ‘नागार्जुन’ और ‘यात्री’ के उपनाम से प्रस्तुत कीं। इनका प्रारंभिक जीवन अभावों का जीवन था। जीवन के अभावों ने ही आगे चलकर इनके संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया।
कवि परिचय : एक दृष्टि में :-
व्यक्तिगत दु:ख ने इन्हें मानवता के दुःख को समझने की क्षमता प्रदान की। जीवन की विषम अनुभूतियां रागिनी बनकर इनकी काव्य रचनाओं में मुखर हुई।
इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। देश विदेश की यात्रा करते हुए यह श्रीलंका पहुंच गये और वहां पाली भाषा के आचार्य बन गए। स्वाध्याय से ही इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने रेणु जी के साथ आपातकाल में जेल यात्रा भी की। नागार्जुन ने सन् 1945 ई० के आसपास साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया। इस संघर्षशील कवि का 5 नवंबर,1998 ई० को स्वर्गवास हो गया।
साहित्यिक परिचय :-
नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि थे। इनके हृदय में दलित वर्ग के प्रति सदैव संवेदना रही थी। अपनी कविताओं द्वारा वे अत्याचार पीड़ित, दुःखी व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके ही संतुष्ट नहीं हो गए,वरन् इन्हें अनीति और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी देते थे। सम-सामयिक राजनीति तथा सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने पर्याप्त मात्रा में लेखन किया। व्यंग्य करने में इन्हें तनिक भी संकोच नहीं था। तीखी और सीधी चोट करने वाले नागार्जुन वर्तमान युग के प्रमुख व्यंगकार थे।
कृतियां :-
नागार्जुन कवि होने के साथ-साथ श्रेष्ठ उपन्यासकार भी हैं। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं-
‘युगधारा’, ‘प्यासी पथराई आंखें’, ‘खून और शोले’ और ‘सतरंगे पंखोंवाली’। ‘भस्मांकुर’ इनका प्रसिद्ध खंडकाव्य है।
काव्यगत विशेषताएं :-
नागार्जुन एक जनवादी कवि हैं, अतः इनका काव्य मानव जीवन संबद्ध है। कुछ रचनाओं में इन्होंने सामाजिक विषमताओं तथा राजनीतिक विद्रूपताओं का व्यंग्य किया है। इस प्रकार प्रगतिवादी विचारधारा के साथ-साथ प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण किया है। अन्यत्र ये प्रकृति वर्णन में भी रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। इनके समूचे काव्य में देश प्रेम की भावना विद्यमान है।
उन्होंने अपने काव्य में समाज में व्याप्त बुराइयों, विषमता, जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपने काव्य में गरीब, शोषित एवं पीड़ित जनता के दुःखों का चित्रण किया है। “अकाल और उसके बाद” कविता में अभाव की स्थिति का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है–
‘’कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास
कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उनके पास
कई दिनों तक लगी भीत पर, छिपकलियों की गश्त,
कई दिनों तक चूहों को भी, हालत रही शिकस्त’’।
जनवादी दृष्टिकोण :-
नागार्जुन की कविताएं समाज के ठोस धरातल पर चलती हैं। उनकी कविताएं कल्पना लोक में विचरण नहीं करती। उन्होंने अपने दुःख के भीतर साधारण लोगों के दुःखों को देखा है और उन्हें अपनी कविताओं में वाणी दी है। सर्वहारा वर्ग की व्यथा एवं पीड़ा को भी अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। जनसाधारण के प्रति सहानुभूति उनके काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। नागार्जुन भी अभावग्रस्त लोगों के पक्षधर बनकर सामने आए। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कविताओं में नगर और गांव की गरीब जनता का चित्रण किया है। उन्होंने उन्हें एक स्थान पर लिखा है–
“कैसे लिखूं शांति की कविता
अमन-चमन को कैसे कड़ियों में बांधू’’।
सम्मान और पुरस्कार :-
नागार्जुन को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनके ऐतिहासिक मैथिली रचना “पत्रहीन नग्न गाछ’’ के लिए 1969 में नवाजा गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलों के रूप में नामांकित कर सम्मानित भी किया था।
देश प्रेम की भावना :-
नागार्जुन की अधिकांश कविताओं में देश प्रेम का स्वर विद्यमान है। इसलिए वे वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। ‘दर्पण और शपथ’ उनकी ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें राष्ट्रीयता का स्वर सुनाई पड़ता है। ‘महा शत्रुओं की दाल न गलने देंगे’ कविता में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त किया है। कवि देश के कण-कण से प्यार करता है–
खेत हमारे, भूमि हमारी, सदा देश हमारा है
इसीलिए तो हमको इसका चप्पा-चप्पा प्यारा है।
भाषा :-
नागार्जुन की रचनाओं को किसी काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इन्होंने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति अपनी कविता को भी स्वतंत्र रखा है। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। कहीं-कहीं इनकी कविता में संस्कृत के क्लिष्ट तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। नागार्जुन ने अपनी कविता में चुने हुए प्रतीकों का प्रयोग किया और उन प्रतीकों के माध्यम से विषय को बड़ी पटुता से उभारा है।
शैली :-
नागार्जुन ने अपने काव्य में मुक्तक और व्याख्यात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। लघु-से-लघु और दीर्घ-से-दीर्घ एक हजार पंक्तियों तक की कविता इनके काव्य में मिलती है। इनकी शैली शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित है। इसके अतिरिक्त इनकी शैली में पात्रानुरूपता, रसानुरूपता, सरलता आदि गुण भी विद्यमान हैं। इनके काव्य में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, संवादात्मक, उद्बोधनात्मक आदि शैलियों के भी दर्शन होते हैं। नागार्जुन का जैसा भाषा शैली पर अधिकार है, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं।
हिंदी साहित्य में स्थान :-
नागार्जुन हिंदी साहित्य की अमर प्रतिभा हैं। सूर्य की विमल और तीक्ष्ण रश्मियों की तरह इनकी कविता जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रकाश कर हुई जगत् के कोने-कोने का स्पर्श करती है। नागार्जुन अपने निर्भीक विचार, स्पष्टवादिता, तीव्र गहन व्यंग्यात्मकता के कारण हिंदी-साहित्य जगत में सदैव स्मरणीय रहेंगे।
नागार्जुन जी के पद :-
बादल को घिरते देखा है
अमल धवल गिरि के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है।
छोटे-छोटे मोती जैसे, अतिशय शीतल वाणी कणों को
मानसरोवर के उन स्वर्णिम-कमलों पर गिरते देखा है।
तुंग हिमाचल के कंधों पर छोटी-बड़ी कई झीलों के
श्यामल शीतल अमल सलिल में
समतल देशों से आ-आकर
पावस की ऊमस से आकुल
तिक्त मधुर बिसतंतु खोजते, हंसो को तिरते देखा है।
एक दूसरे से वियुक्त हो
अलग-अलग रहकर ही जिनको
सारी रात बितानी होती–
निशा काल के चिर अभिशापित
बेबस, उन चकवा-चकई का,
बंद हुआ क्रन्दन फिर उनमें
उस महान् सरवर के तीरे
शैवालों की हरी दरी पर, प्रणय-कलह छिड़ते देखा है।
कहां गया धनपति कुबेर वह,
कहां गई उसकी वह अलका?
नहीं ठिकाना कालिदास के,
व्योम-वाहिनी गंगाजल का!
ढूंढ़ा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर!
कौन बताए वह यायावर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर!
जाने दो, वह कवि कल्पित था,
मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर
महामेघ को झंझानिल से, गरज-गरज भिड़ते देखा है।
FAQ Questions :-
प्रश्न - कवि नागार्जुन के बचपन का नाम क्या है?
उत्तर - नागार्जुन के बचपन का नाम ‘ठक्कन मिसर’ था।
प्रश्न - नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं?
उत्तर - अभिनंदन (नागार्जुन की रचना), अन्न हीनम क्रियानम।
प्रश्न - नागार्जुन क्यों प्रसिद्ध था?
उत्तर - नागार्जुन एक भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता के सिद्धांत को स्पष्ट किया और परंपरागत रूप से उन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है।
प्रश्न - नागार्जुन ने किसकी खोज की थी?
उत्तर - कुछ प्रमाणों के अनुसार वे ‘अमरता’ की प्राप्ति की खोज करने में लगे हुए थे और उन्हें पारा तथा लोहा के निष्कर्षण का ज्ञान था।
प्रश्न - अचार्य नागार्जुन की मृत्यु कैसे हुई?
उत्तर - नागार्जुन वास्तव में सहमत थे, लेकिन कुमार तलवार से उनका सर नहीं काट सकते थे। नागार्जुन ने कहा कि पिछले जन्म में उन्होंने घास काटते समय एक चींटी को मार डाला था। कर्म के परिणाम स्वरुप, उसका सर केवल कुशा घास के एक ब्लेड से ही काटा जा सकता था। कुमार ने ऐसा किया और नागार्जुन की मृत्यु हो गई।
इसे भी पढ़ें 👇👇👇
• भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी
• आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी
• सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय
• केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय
• हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय
• सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय
• शिवमंगल सिंह सुमन का जीवन परिचय
• डॉ संपूर्णानंद का जीवन परिचय
• राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय
यह Blog एक सामान्य जानकारी के लिए है इसका उद्देश्य सामान्य जानकारी प्राप्त कराना है। इसका किसी भी वेबसाइट या Blog से कोई संबंध नहीं है यदि संबंध पाया गया तो यह एक संयोग समझा जाएगा।
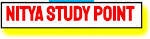

Post a Comment