भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं भाषा शैली || Jivan Parichay in Hindi
भारतेंदु हरिश्चंद्र
(जीवनकाल : सन् 1850 - 1885 ई०)
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय यहां पर सबसे सरल भाषा में लिखा गया है। यह जीवन परिचय कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के सभी पहलुओं के विषय में चर्चा की गई है, तो इसे कोई भी व्यक्ति भी पढ़ सकता है।
जीवन परिचय -
युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभासंपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन् 1850 ईसवी में, काशी में हुआ था। इनके पिता गोपालचंद्र 'गिरिधरदास' बृज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता-पिता के सुख से वंचित हो गए थे।
कवि परिचय : एक दृष्टि में
भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने 'क्वींस कॉलेज' में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रूचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका; परिणामस्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य-रचना के अतिरिक्त इनकी रूचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय में ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे।
भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हरसंभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन् 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया।
साहित्यिक परिचय –
भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य-रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये बृज भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाएं हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य-साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक 'विद्यासुंदर' का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया।
सन् 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी 'कवि-वचन-सुधा' नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष उपरांत सन् 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका 'हरिश्चंद्र मैगजीन' का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम 'हरिश्चंद्र-चंद्रिका' हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुत: हिंदी-गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है।
भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रावृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य-रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा-निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन् 1880 ई० में इन्हें 'भारतेंदु' की उपाधि से सम्मानित किया।
कृतियां – अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोष प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं–
नाटक – भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार हैं –
(क) मौलिक – सत्य हरिश्चंद्र, नीलदेवी, श्री चंद्रावली, भारत-दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम्, सती-प्रताप तथा प्रेम-जोगिनी।
(ख) अनूदित – मुद्राराक्षस, रत्नावली, भारत-जननी, विद्यासुंदर, पाखंड-विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूरमंजरी, धनंजय-विजय।
निबंध संग्रह – सुलोचना, परिहास-वंचक, मदालसा, दिल्ली-दरबार-दर्पण, लीलावती।
इतिहास – कश्मीर-कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति।
यात्रा वृतांत – सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि।
जीवनियां – सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मुहम्मद आदि।
भाषा-शैली -
भाषा – भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी-भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी हिंदी-भाषा को स्थायीत्व प्रदान किया। उन्होंने इसे जनसामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोकभाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू-फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा के प्रति जन-सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई।
शैली – भारतेंदु जी गद्य-शैली व्यवस्थित और सजीव है। इनकी गद्य-शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। उनमें जटिलता के स्थान पर प्रवाह देखने को मिलता है। भारतेंदु जी ने निम्नलिखित शैलियों का उपयोग किया–
वर्णनात्मक शैली – अपने वर्णनप्रधान निबंधों एवं इतिहास-ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाक्यों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों से युक्त उनकी वर्णनात्मक शैली की अपनी अलग मौलिकता है।
विवरणात्मक शैली – भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा-संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी यह शैली कवित्तपूर्ण आभा से मंडित है।
विचारात्मक शैली – 'वैष्णवता और भारतवर्ष', 'भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है?' आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विवरणात्मक शैली का परिचय मिलता है। इस शैली पर आधारित रचनाओं में इनके विचारों की गंभीरता एवं विश्लेषण-शक्ति के दर्शन होते हैं।
भावात्मक शैली – भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवनी-साहित्य एवं कई नाटकों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें इनके भावपक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है।
व्यंग्यात्मक शैली – भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंधों, नाटकों आदि में यत्र-तत्र व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन भी होते हैं।
हास्य शैली – भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हास्य शैली में भी रचनाएं की हैं। हास्य शैली में लिखी गई इनकी रचनाओं में 'अंधेर नगरी', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' उल्लेखनीय हैं। इनके निबंधों में भी यत्र-तत्र हास्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है।
इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शोध शैली, भाषण शैली, स्रोत शैली, प्रदर्शन शैली एवं कथा शैली आदि में भी निबंधों की रचना की है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताएं -
भारतेंदु की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। इन्होंने युग की आवश्यकता तथा जन रुचि को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की साहित्य रचना की है। उनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से उनका काव्य उच्च कोटि का है इनके काम में मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं -
भाव पक्ष -
भारतेंदु जी के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम था। भारतवर्ष का गौरव प्रदर्शित करते हुए वे अपने 'भारत दुर्दशा' नाटक में कहते हैं -
"भारत के भुजबल जग रच्छित, भारत विद्या ज्योति जन सिंचित। भारत तेज जगत विस्तारा, भारत-भय कंम्पित संसारा ।।"
विषय की नवीनता -
श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने बहुत स्वाभाविक वर्णन किया है। उनका विरह वर्णन तो बहुत ही अनूठा है। भक्ति के क्षेत्र में भक्तिकालीन साहित्य से वे बहुत प्रभावित हैं। भारतेंदु जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रीतिकालीन श्रृंगारिक भावना का विरोध कर देशप्रेम और समाज सुधार की भावना को अपने काव्य का विषय बनाया। अपने 'अंधेर नगरी' और 'भारत दुर्दशा' नाटक में इन्होंने सामाजिक कुरीतियों और भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग्य कसे हैं। अछूतोद्धार तथा नवजागरण की भावना भी इनके काव्य में जहां-तहां पाई जाती है।
कला पक्ष -
भारतेंदु जी ने कविता में पूर्व प्रचलित भाषा का ही प्रयोग किया किंतु गद्य में इन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। ब्रजभाषा से इन्होंने आप्रचलित शब्दों को निकाल कर उसे सर्वथा व्यवहारोपयोगी बना दिया। प्रचलित उर्दू शब्दों पालिसी, मेडल आदि अंग्रेजों के प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा में प्रभाव तथा चमत्कार उत्पन्न हो गया मुहावरेदार भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है -
"काले परे कोस चलि चलि थकि गये पॉय सूखे के कासाले परे ताले परे नस के। रोय रोय नैननि में हाले पड़े, जाले परे, मदन के पाले परे, प्रान पर बस के,
हरिश्चंद्रगड अंगहू हवाले परे रागन के,
सोगन के भाले परे तन बल खटके।
पगन में छाले परे नाघिंबे को नाले परे,
तऊ लाल-लाल परे, रावरे दरस के ।।"
हिंदी-साहित्य में स्थान –
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी-भाषा और हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें 'आधुनिक हिंदी गद्य-साहित्य का जनक', 'युग निर्माता साहित्यकार' अथवा 'आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक' कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युगद्रष्टा, युगस्त्रष्टा, युग-जागरण के दूत और एक युग-पुरुष के रूप में जाना जाता है।
साहित्य में योगदान -
निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बाबू हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थे। इन्होंने समाज और साहित्य का प्रत्येक कोना झांका है। अर्थात् साहित्य के सभी क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है किंतु यह खेद का ही विषय है कि 35 वर्ष की अल्पायु में ही वे स्वर्गवासी हो गए थे यदि ऐसा ना होता तो संभवत हिंदी साहित्य का कहीं और ज्यादा विकास हुआ होता। यह उनके व्यक्तित्व की ही विशेषता थी कि वे कवि, लेखक, नाटककार साहित्यकार एवं संपादक सबकुछ थे। हिंदी साहित्य को पुष्ट करने में आपने जो योगदान प्रदान किया है। वह सराहनीय है तथा हिंदी जगत आपकी सेवा के लिए सदैव ऋणी रहेगा। इन्होंने अपने जीवन काल में लेखन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया। अभी तो 35 वर्ष की अल्पायु में ही ब 72 ग्रंथों की रचना करना संभव हो सकता था। इन्होंने छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अपने कार्यों से इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सदा के लिए स्थाई रूप से स्थान बनाया है। अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण ही यह आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कहे जाते हैं पंत जी ने इनके बारे में ठीक ही कहा है -
भारतेन्दु कर गये,
भारती की विणा निर्माण।
किया अमर स्पर्शों में,
जिसका बहु विधि स्वर संधान।
आता यही कहा जा सकता है कि बाबू हरिश्चंद्र (भारतेंदु हरिश्चंद्र) जी हिंदी साहित्य के आकाश के एक देदीप्यमान नक्षत्र थे। उनके द्वारा हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है।
भारतेंदु जी की मृत्यु -
शरीर के अस्वस्थ होने एवं अनेक चिंताओं के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में 1885 को भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया।
गद्य शैली का निर्धारण -
भारतेंदु जी से पहले हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था, हिंदी गद्य की कोई निर्धारित शैली भी नहीं थी। एक और राजा शिवप्रसाद 'सितारे-हिंद' की उर्दू प्रधान शैली थी तो दूसरी ओर थी राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ शुद्ध भाषा शैली। यह दोनों ही हिंदी जगत में मान्य ना हो सके। भारतेंदु जी ने मध्यम मार्ग अपनाया और हिंदुस्तानी खड़ी बोली को हिंदी गद्य की आदर्श भाषा शैली के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी शैली में ना अरबी फारसी के शब्दों की भरमार थी, ना संस्कृत शब्दों का आग्रह था। उनकी भाषा शैली में ना 'सितारे-हिंद' का उर्दूपन। ना राजा लक्ष्मणसिंह की संस्कृतनिष्ठता। वास्तव में इन्होंने एक ऐसी सर्वमान्य शैली का प्रयोग किया जो हिंदी गद्य साहित्य के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुई। गद्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था।
विविध गद्य विधाओं का आविर्भाव -
भारतेंदु जी का समय हिंदी गद्य साहित्य के आविर्भाव का काल था। भारतेंदु जी ने हिंदी में नाटक, निबंध, कहानी तथा जीवनी आदि विविध गद्य विधाओं को जन्म दिया। उन्होंने स्वयं लिखा और दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित किया। इनके मित्रों ने भी हिंदी भाषा के विकास में उन्हें सहयोग दिया। अनेक नाटक, निबंध, उपन्यास तथा कहानियां इस काल में लिखे गए। विविध गद्य विधाओं से हिंदी साहित्य का भंडार भरा गया। उनके मित्रों और सहयोगियों का एक बड़ा समुदाय बन गया जिसे "भारतेंदु मंडल" के नाम से ही जाना गया। यही कारण है कि भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है।
समाज सेवा -
साहित्य सेवा के साथ-साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती थी। उन्होंने कई समस्याओं की स्थापना में अपना योगदान दीन-दुखियों साहित्य तथा मित्रों की सहायता करना भी अपना कर्तव्य समझते थे। धन की अत्याधिक व्यय से भारतेंदु जी त्रणी बन गए और चिंता के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया। परिणाम स्वरूप 1885 में अल्पायु में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस्त लिया।
मौलिक नाटक -
• वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति।
• सत्य हरिश्चंद्र
• श्री चंद्रावली
• विषस्य विषमौषधम्
• भारत दुर्दशा
• नील देवी
• अंधेर नगरी
• प्रेम जोगिनी
• सती प्रताप (1883, अपूर्ण, केवल चार दृश्य, (गीतिरूपक, बाबूराधाकृष्ण दास ने पूर्ण किया)
निबंध संग्रह -
• नाटक
• कालचक्र जर्नल
• लेवी प्राण लेवी
• भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है?
• कश्मीर कुसुम
• जातीय संगीत
• संगीत सार
• हिंदी भाषा
• स्वर्ण में विचार सभा
काव्य कृतियां -
• भक्तसर्वस्व
• प्रेम मालिका
• प्रेम माधुरी
• प्रेम तरंग
• उत्तरार्द्ध भक्तमाल
• प्रेम प्रलाप
• होली
• मधु मुकुल
• राग संग्रह
• वर्षा विनोद
• विनय प्रेम पचासा
• फूलों का गुच्छा खड़ीबोली - काव्य
• प्रेम फुलवारी
• कृष्ण चरित्र
• दानलीला
• तन्मय लीला
• नए जमाने की मुकरी
• सुमनांजलि
• बंदर सभा हास्य व्यंग
• बकरी विलाप हास्य व्यंग
कहानी -
• अद्भुत अपूर्व स्वप्न
यात्रा वृतांत -
• सरयूपार की यात्रा
• लखनऊ
• आत्मकथा
• एक कहानी - कुछ आप बीती, कुछ जग बीती
उपन्यास -
• पूर्णप्रकाश
• चंद्रप्रभा
FAQ'S -
1. भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कैसे लिखें ?
उत्तर - युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभासंपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन् 1850 ईसवी में, काशी में हुआ था। इनके पिता गोपालचंद्र 'गिरिधरदास' बृज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही ये माता-पिता के सुख से वंचित हो गए थे।
2. हिंदी भाषा के जन्मदाता कौन है?
उत्तर - आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके खून मे था हास्य व्यंग।
3. भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था?
उत्तर - भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था।
4. भारतेंदु हरिश्चंद्र कुल कितने नाटक लिखे?
उत्तर - उन्होंने मैलिक और अनुदेश मिलाकर कुल 17 नाटकों की रचना की। भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में रहा। इनके नाटक लेखन की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से हुईं।
5. भारतेंदु हरिश्चंद्र का कलम नाम क्या है?
उत्तर - इन्होंने छद्म नाम गिरिधरदास के तहत लिखा। एक लेखक संरक्षक और आधुनिकीकरण कर्ता के रूप में इनकी सेवाओं के सम्मान में 1880 में काशी के विद्वानों द्वारा एक सार्वजनिक बैठक में उन्हें भारतेंदु भारत का चंद्रमा शीर्षक दिया गया।
6. भारतेंदु ने कितने ग्रंथ लिखे हैं?
उत्तर - भारतेंदु निम्नलिखित ग्रंथ लिखे हैं - अंधेर नगरी चौपट राजा, दुर्लभ बंधु, भारत दर्शन आदि।
7. भारतेंदु युग के लेखक कौन है?
उत्तर - भारतेंदु युग के प्रमुख कवि - भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, आदि इस युग के प्रमुख कवि थे।
8. भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है?
उत्तर - भारतेंदु काल को नवजागरण काल भी कहा गया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को संक्रांति काल के दो पक्ष हैं।
9. भारतेंदु का मतलब क्या होता है?
उत्तर - भारतेंदु नाम का अर्थ बेहद अलग है। भारतेंदु नाम का अर्थ है 'भारत का चांद'.
10. भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था?
उत्तर - भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ उनका मूल नाम हरीश चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी थिएटर के भी पितामह कहे जाते हैं। उनके पिता गोपाल चंद एक कवि थे।
इसे भी पढ़ें - 👉👉
• भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी
• आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी
• सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय
यह Blog एक सामान्य जानकारी के लिए है इसका उद्देश्य सामान्य जानकारी प्राप्त कराना है। इसका किसी भी वेबसाइट या Blog से कोई संबंध नहीं है यदि संबंध पाया गया तो यह एक संयोग समझा जाएगा।
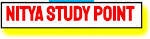



Post a Comment