सूरदास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली एवं रचनाएं || Surdas ka Jivan Parichay
जीवन काल : सन् 1478 - 1583 ई०
जीवन परिचय -
सूरदास के जन्म स्थान एवं जन्मतिथि के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म वैशाख सुदी संवत् 1535 (सन् 1478 ई०) में स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में संवत् 1540 में मानते हैं। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म-स्थल मानते हैं।
कवि परिचय : एक दृष्टि में
इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि प्रकृति तथा बाल-मनोवृत्तियों एवं मानव-स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध कदापि नहीं कर सकता।
सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गऊघाट पर श्रीनाथजी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था तथा विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर कृष्ण-लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने 'श्रीकृष्ण गीतावली' की रचना की थी।
सूरदास जी की मृत्यु संवत् 1640 (सन् 1583 ई०) में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी।
साहित्यिक परिचय -
हिंदी काव्य-जगत में सूरदास कृष्णभक्ति की अगाध एवं अनंत भाव धारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य 'श्रीमद्भागवद्' से अत्यधिक प्रभावित रहा है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल-भाव एवं वात्सल्य-भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, उसका उदाहरण विश्व-साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। 'भ्रमरगीत' में इनके विरह-वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास के 'भ्रमरगीत' में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव प्रकट हुआ है, वह इनकी महान् काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है।
सूरदास जी की शिक्षा –
सूरदास ने अपने जीवन काल में सूरसागर, सूर-सारावली, साहित्य लहरी नामक रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। उनके इस उपाधि पर एक दोहा प्रसिद्ध है–
सूर सूर तुलसी ससी,उडुगन केशवदास।
अब के कवि खद्योत सम, जहँ-तहँ करत प्रकाश।।
कृतियां -
भक्त-शिरोमणि सूरदास ने लगभग सवा लाख पदों की रचना की थी। 'नागरी प्रचारिणी सभा, काशी' की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके तीन ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं-
सूरसागर - 'सूरसागर' एकमात्र ऐसी कृति है, जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके सवा लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। 'सूरसागर' पर 'श्रीमद्भागवद्' का प्रभाव है। संपूर्ण 'सूरसागर' एक गीतिकाव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं।
सूरसारावली - यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथावस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1,107 छंद हैं।
साहित्य लहरी - 'साहित्यलहरी' में सूरदास के 118 दृष्टकूट-पदों का संग्रह है। 'साहित्यलहरी' में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं-कहीं पर श्री-कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हुआ है तथा एक दो स्थानों पर 'महाभारत' की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है।
इसके अतिरिक्त 'गोवर्धन-लीला', 'नाग-लीला', 'पद-संग्रह' एवं 'सूर-पचीसी' ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं।
काव्यगत विशेषताएं
(अ) भाव पक्ष
हिंदी साहित्य में सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। इन्होंने अपने काव्य में श्रीकृष्ण की विविध बाल-लीलाओं की सुंदर झांकी प्रस्तुत की हैं। माता यशोदा का उन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हठ करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि विविध प्रसंगों को सूर ने अत्यंत तन्मयता तथा रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है।
श्रृंगार वर्णन में भी सूरदास जी को अद्भुत सफलता मिली है। इन्होंने अपने काव्य में राधा-कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा और श्रीकृष्ण के परिचय का यह चित्र देखिए-
बूझत स्याम कौन तू गोरी।
कहां रहत काकी तू बेटी? देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी।।
संयोग के साथ सूर ने वियोग के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियां, राधा, यशोदा, गोप, पशु-पक्षी एवं ब्रज के सभी जड़ चेतन उनके बिरह में व्याकुल हो उठते हैं। यहां तक कि संयोग की स्थितियों में सुख प्रदान करनेवाली कुंजी जैसी सभी वस्तुएं वियोग के क्षणों में दुखदायक बन जाती हैं। यथा -
बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजैं।
सूरदास जी की भक्ति सखा-भाव की है। इन्होंने श्रीकृष्ण को अपना मित्र माना है। सच्चा मित्र अपने मित्र से कोई पर्दा नहीं रखता और ना ही किसी प्रकार की शिकायत करता है। सूर ने बड़ी चतुराई से काम लिया है। सूर की भक्ति-भावना में अनन्यता, निश्छलता एवं पावनता विद्यमान है।
सूरदास जी के काव्य में प्रकृति का प्रयोग कहीं पृष्ठभूमि रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में और कहीं अलंकारों के रूप में किया गया है। गोपियों के विरह वर्णन में प्रकृति का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया गया है।
(ब) कलापक्ष
भाषा -
सूर की भाषा भावप्रधान, सरल सुबोध एवं सशक्त है। इनकी शब्द योजना भी सराहनीय है। चूंकि सूरदास जी का एक उद्देश्य ब्रजभाषा को सर्वमान्य साहित्यिक भाषा बनाना भी था, इसलिए इन्होंने तत्सम, तद्भव और ठेठ शब्दों के साथ-साथ विदेशी शब्दों को भी अपनाया है। सूर काव्य में मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों की भी अधिकता है तथा कहीं भी इनका प्रयोग बिना किसी प्रयोजन के नहीं हुआ है। सूर की भाषा में प्रवाह के साथ ओजगुण भी है। साथ ही माधुर्य और प्रसाद गुण भी दिखाई देता है। सूर ने काव्य में अलंकारों का स्वभाविक प्रयोग किया है। इनमें कृतिमता कहीं नहीं है। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत तथा अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है।
शैली -
सूरदास जी ने अपने काव्य में विविध शैलियों का प्रयोग किया है। इनमें प्रमुख हैं-
चित्रात्मक शैली - सूरदास जी ने अपने काव्य में इस शैली का प्रयोग किया है। ये जिस दृश्य का वर्णन करते हैं उसका एक चित्र-सा उपस्थित कर देते हैं। सूर के काव्य में विविध प्रकार के चित्र मिलते हैं, जैसे रूप चित्र, भाव चित्र, स्वभाव चित्र आदि।
वर्णनात्मक शैली - सूरदास जी ने वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग अधिकांशतः कथा-वर्णन में किया गया है। कहीं-कहीं दृष्टकूट पदों में शैली क्लिष्ट हो गई है। सूर ने मुक्तक काव्य-शैली को अपनाया है। समग्रत: उनकी शैली सरल एवं प्रभावशाली है।
सूर ने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छप्पय, सवैया तथा घनाक्षरी आदि विविध प्रकार के परंपरागत छंदों का प्रयोग किया है।
हिंदी साहित्य में स्थान -
महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वाग्धारा के रूप में भक्ति-श्रंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं में बंधकर प्रवाहित होती आ रही थी उसे सूर ने जन-भाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही ब्रज भाषा के साहित्य में सूर का है। इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर (सूर्य) कहा गया है।
दोहे -
अब कैं राखि लेहु भगवान |
हौं अनाथ बैठ्यौ द्रुम-डरिया, पारधि साधे बान || ताकैं डर मैं भाज्यौ चाहत, ऊपर दुक्यौ सचान | दुहूँ भाँति दुख भयौ आनि यह, कौन उबारै प्रान ? सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी, कर छूट्यौ संधान | सूरदास सर लग्यौ सचानहि, जय-जय कृपानिधान ||
मेरौ मन अनत कहाँ सुख पावै ||
जैसे उड़ि जहाज कौ पंछी, फिरि जहाज पर आवै ||
कमल- नैन कौ छाँड़ि महातम, और देव को ध्यावै |
परम गंग कौ छाँड़ि पियासौ, दुरमति कूप खनावै ||
जिहिं मधुकर अंबुज-रस चाख्यौ, क्यौं करील-फल भावै |
सूरदास-प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावै ||
ऊधौ मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं |
हंस-सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंज़नि की छांहीं ||
वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाहीं | ग्वाल-बाल मिलि करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाहीं ||
यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि-मुक्ताहल जाहीं | जबहिं सुरति आवति वा सुख की, जिय उमागत तन नाहीं ||
अनगन भाँति करि बहु लीला, जसुदा नन्द निबाहीं |
सूरदास प्रभु रहे मौन ह्रै, ये कहि-कहि पछिताहीं ||
बिनु गुपाल बैरिनि भई कुंजैं ।
तब वै लता लगति तन सीतल, अब भइँ विषम ज्वाल की पुंजै ||
बृथा बहति जमुना खग बोलत, बृथा कमल-फूलनि अलि गुंजैं |
पवन, पान, घनसार, सजीवन, दधि-सुत किरनि भानु भई भुंजै ||
यह ऊधौ कहियौ माधौ सौं, मदन मारि कीन्हीं हम लुंजैं |
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस कौं, मग जोवत अँखियाँ भई छुंजैं ||
हमारैं हरि हारिल की लकरी ।
मन क्रम बचन नंद-नंदन उर, यह दृढ़ करि पकरी |
जागत-सोवत स्वप्न दिवस-निसि, कान्ह कान्ह जकरी |
सुनत जोग लागत है ऐसौ, ज्यौं करुई ककरी ||
सु तौ व्याधि हमकौं ले आए, देखी सुनी न करी | यह तौ सूर तिनहिं लै सौंपौ, जिनके मन चकरी ||
ऊधौ जोग जोग हम नाहीं |
अबला, सार- ज्ञान कहं जानै, कैसें ध्यान धराहीं || तेई मूंदन नैन कहत हौ, हरि मूरति जिन माहीं |
ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमतैं सुनी न जाहीं ||
श्रवण चीरि सिर जटा बंधावहु, ये दुःख कौन समाहीं |
चंदन तजि अंग भस्म बतावत, बिरह-अनल अति दाहीं ||
जोगी भ्रमत जाहि लगि भूले, सो तौ है अप माहीं |
सूर स्याम तैं न्यारी न पल-छिन, ज्यों घट तैं परछाहीं ||
लरिकाई कौ प्रेम कहौ अलि, कैसे छूटत ?
कहा कहौं ब्रजनाथ चरित, अंतरगति लूटत ||
वह चितवनि वह चाल मनोहर, वह मुसकानि मंद-धुनि गावनि |
नटवर भेष नंद-नंदन कौ वह विनोद वह बन तैं आवनि ||
चरन कमल की सौंह करति हौं, यह संदेस मोहिं विष सम लागत |
सूरदास पल मोहिं न विसरति, मोहन मूरति, सोवत जागत ||
कहत कत परदेसी की बात |
मंदिर अरध अवधि बदि हमसौं, हरि अहार चलि जात ||
ससि रिपु बरष, सूर रिपु जुग बर, हर-रिपु कीन्हौं घात |
मघ पंचक लै गयौ सांवरौ, तातैं अति अकुलात || नखत, बेद, ग्रह, जोरि, अर्ध करि, सोइ बनत अब खात |
सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजैं पछितात ||
निसि दिन बरषत नैन हमारे |
सदा रहति बरसा ऋतु हम पर, जब तैं स्याम सिधारे ||
दृग अंजन न रहत निसि बासर, कर कपोल भए कारे |
कंचुकि-पट सूखत नहिं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे ||
आँसू सलिल सबै भइ काया, पल न जात रिस टारे |
सूरदास-प्रभु यहै परेखौ, गोकुल काहैं बिसारे ||
ऊधौ भली भई ब्रज आए |
बिधि कुलाल कीन्हें काँचे घट ते तुम आनि पकाए |
रंग दीन्हौं हो कान्ह सांवरैं, अँग-अँग चित्र बनायें | पातैं गरे न नैन नेह तैं, अवधि अटा पर छाए || ब्रज करि अंवा जोग ईधन करि, सुरति आनि सुलगाए |
फूंक उसास बिरह प्रजरनि संग, ध्यान दरस सियराए ||
भरै संपूरन सकल प्रेम-जल छुवन न काहू पाए | राज काज तैं गए सुर प्रभु, नन्दनन्दन कर लाए ||
अँखियाँ हरि दर्शन की भूखीं |
कैसैं रहति रूप-रस राँची, ये बतियाँ सुनि रूखीं ||
अवधि गनत, इकटक मग जोवत, तब इतनौ नहिं झूखीं |
अब यह जोग सँदेसौ सुनि सुनि, अति अकुलानी दूखीं ||
बारक वह मुख आनि दिखावहु, दुहि पय पिबत पतूखीं |
सूर सुकत हठि नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखीं ||
सूरदास का राजघराने से संबंध -
महाकवि सूरदास के भक्ति में गीतों की गूंज चारों तरफ फैल गई थी। जिसे सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं पर मुग्ध हो गए थे। जिसने उनके काम से प्रभावित होकर अपने यहां रख लिया था। आपको बता दें कि सूरदास के काव्य की ख्याति बनने के बाद हर कोई सूरदास को पहचानने लगा। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम दिनों को सूरदास ने ब्रज में व्यतीत किया, जहां रचनाओं के बदले उन्हें जो भी प्राप्त होता। उसी से सूरदास अपना जीवन बसर किया करते थे।
सूरदास की काव्यगत विशेषताएं-
सूरदास जी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जी अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। और उपमाओ की बाढ़ आ जाती है। और रूपकों की बारिश होने लगती है। साथ ही सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्ति को श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया था। साथ ही सूरदास जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का भी जीवंत उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं सूरदास जी ने काव्य और कृष्ण भक्ति का जो मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया, वह अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता।
सूरदास की मृत्यु कब हुई -
मां भारती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास स्थित पारसौली गांव में सदैव के लिए दुनिया से विदा हो गए। सूरदास जी ने कब की धारा को एक अलग ही गति प्रदान की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य और पद्य के क्षेत्र में भक्ति और श्रृंगार रस का बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया है। और हिंदी कब के क्षेत्र में उनकी रचना एक अलग स्थान रखती हैं। साथ ही ब्रजभाषा को साहित्य दृष्टि से उपयोगी बनाने का श्रेय महाकवि सूरदास को ही जाता है।
क्या सूरदास जन्म से अंधे थे? -
सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अभी मतभेद हैं। सुधारने तो अपने आप को जन्मांध बताया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रंगार रूपी राधा और गोपियों का सजीव चित्रण किया है। आंखों से साक्षात देखे बगैर नहीं हो सकता। विद्वानों का मानना है कि वह जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी के अलौकिक रूप का बहुत ही मनोनीत रूप से वर्णन किया है। उन्होंने आत्मग्लानिवश, क्या चने रूप से अथवा किसी और कारण अपने आप को जन्मांध बताया हो।
अंधे होने की कहानी -
उनके अंधे होने की कहानी भी प्रचलित है। कहानी कुछ इस तरह है कि सूरदास ( मदन मोहन ) एक बहुत ही सुन्दर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे वह हर दिन नदी किनारे जाकर बैठ जाता और गीत लिखता एक दिन एक ऐसा वाक्य हुआ जिससे उसका मन को मोह लिया।
हुआ यूं कि एक सुंदर नवयुग की नदी किनारे कपड़े धो रही थी, मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस वीडियो को देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो जमुना किनारे राधिका स्नान कर बैठी हो। उसने युवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास आकर बोली आप मदन मोहन जी हो ना? तो वे बोले हां मैं मदन मोहन हूं। कविताएं लिखता हूं तथा गाता हूं आपको देखा तो रुक गया। युवती ने पूछा क्यों? तो वह बोले आप हो ही इतनी सुंदर। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। और सुंदर युवती का चेहरा और उनके सामने से नहीं जा रहा था, और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे तभी वह एक शादीशुदा स्त्री आई। मदनमोहन इसके पीछे पीछे चल दिए। जब है उसके घर पहुंचे तो उसके पति ने दरवाजा खोल तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। श्री मदन मोहन ने दो जलती हुई सलाये तथा उसे अपनी आंख में डाल दी। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास।
Frequently Asked Questions (FAQ)-
प्रश्न - सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखे?
उत्तर - महाकवि श्री सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था। यह गांव मथुरा-आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं।
प्रश्न - सूरदास अंधे क्यों हुऐ?
उत्तर - सूरदास के पिता का नाम रामदास गायक था जबकि उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। पुराणों के अनुसार, सूरदास जन्म से ही अंधे थे इसलिए उनके परिवार ने उनका त्याग कर दिया था।
प्रश्न - सूरदास के काव्य का प्रमुख विषय क्या है?
उत्तर - पुष्टिमार्ग में आने के साथ उनका वर्ण्य विषय श्री कृष्ण लीला हो गया। सूरदास मूलतः भक्त कवि हैं। कृष्ण लीला के अंतर्गत वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन उनकी भक्ति भावना के केंद्रीय विषय हैं। इन दोनों ही भावों के महासागर में सूर की पैठ बहुत गहरी है।
प्रश्न - सूरदास की भाषा शैली क्या है?
उत्तर - सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, जिसमें उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ देशज और तद्भव शब्दों का आंशिक रूप से प्रयोग किया है।
प्रश्न - सूरदास की प्रसिद्ध कविता कौन सी थी?
उत्तर - सूरदास को उनकी रचना सूरसागर के लिए जाना जाता है।
प्रश्न - सूरदास की काव्य भाषा क्या है?
उत्तर - महाकवि सूरदास हिंदी के श्रेष्ठ भक्त कवि थे। उनका संपूर्ण का ब्रजभाषा का श्रृंगार है, जिसमें विभिन्न राग, रागिनियों के माध्यम से एक भक्त ह्रदय के भावपूर्ण उद्धार व्यक्ति हुए हैं।
प्रश्न - सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखें?
उत्तर - रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार सूरदास का जन्म संवत 1540 के सन्निकट और मृत्यु संवत् 1620 ईसवी के आसपास मानी जाती है। श्री गुरु बल्लभ तत्व सुनाएं लीला भेद बताइए। सूरदास की आयु सूट सूरावली के अनुसार उस समय 67 वर्ष थी। वे सांसद ब्राह्मण थे और जन्म के अन्य थे।
प्रश्न - सूरदास का जीवन परिचय एवं रचनाएं?
उत्तर - भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म 'रुनकता' नामक ग्राम में 1478 ई० में पंडित राम दास जी के घर हुआ था।
1. सूरसागर- यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीतिकाव्य है, जो 'श्रीमद् भागवत' ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल-लीलाओं, गोपी-प्रेम, गोपी-विरह, उद्धव- गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है।
2. सूरसारावली- यह ग्रंथ सूरसागर का सारभाग है, जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं।
3. साहित्यलहरी- इस ग्रंथ में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं-कहीं श्री कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन तथा एक-दो स्थलों पर 'महाभारत' की कथा के अंशों की झलक भी दिखाई देती है।
प्रश्न - सूरदास का जन्म स्थान?
उत्तर - विद्वान् 'सीही' नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं।
प्रश्न - सूरदास का विवाह?
उत्तर - कहा जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था। हालांकि इनकी विवाह को लेकर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी उनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। कहा जाता है कि संसार से विरक्त होने से पहले सूरदास जी अपने परिवार के साथ ही जीवन व्यतीत किया करते थे।
प्रश्न - सूरदास की मृत्यु कब हुई थी?
उत्तर - मां भारती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास स्थित पारसौली गांव में सदैव के लिए दुनिया से विदा हो गए। सूरदास जी ने कब की धारा को एक अलग ही गति प्रदान की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य और पद्य के क्षेत्र में भक्ति और श्रृंगार रस का बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया है। और हिंदी कब के क्षेत्र में उनकी रचना एक अलग स्थान रखती हैं। साथ ही ब्रजभाषा को साहित्य दृष्टि से उपयोगी बनाने का श्रेय महाकवि सूरदास को ही जाता है।
इसे भी पढ़ें - 👉👉
• भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी
• आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी
• सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय
• डॉ संपूर्णानंद का जीवन परिचय
• राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय
यह Blog एक सामान्य जानकारी के लिए है इसका उद्देश्य सामान्य जानकारी प्राप्त कराना है। इसका किसी भी वेबसाइट या Blog से कोई संबंध नहीं है यदि संबंध पाया गया तो यह एक संयोग समझा जाएगा।
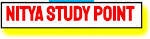


Post a Comment