Aacharya Ramchandra Shukla ka jivan Parichay| आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय
आज की पोस्ट में हम हिंदी साहित्य के चर्चित विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल (Aacharya Ramchandra Shukla) के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे।
- जीवन परिचय -
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय -
संक्षिप्त परिचय
जीवन परिचय:- हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार, "उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।"
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईसवी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' काशी से जुड़कर इन्होंने 'शब्द-सागर' के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया।
शुक्ला जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है।
जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ।
रचनाएं:- शुक्ला जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नांकित हैं-
निबंध:- चिंतामणि (दो भाग), विचार वीथी।
आलोचना:- रसमीमांसा, त्रिवेणी (सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं)।
इतिहास:- हिंदी साहित्य का इतिहास।
संपादन:- तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमरगीत सार, आनंद कादंबिनी।
काव्य रचनाएं:- 'अभिमन्यु वध' , '11 वर्ष का समय' ।
प्रमुख कृतियां - हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नागरी प्रचारिणी पत्रिका।
भाषा शैली:- शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी। वहीं दूसरी ओर अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक बात कहने में सक्षम थे।
हिंदी साहित्य में स्थान:- हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को 'शुक्ल युग' के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरुप हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका।
इसे भी पढ़ें 👉 जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय
यह भी पढ़ें 👉 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय
अन्य - जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादंबरी।
इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी (11 वर्ष का समय ) काव्य कृति (अभिमन्यु वध) की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र (काव्य) आदि प्रमुख है।
शुक्ला जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार उर्दू ,फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ला जी ने मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजना पूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरकर प्रयास किया है।
शुक्ला जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आ पाता । कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक,भावनात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल की प्रसिद्ध है।
प्रस्तुत मित्रता निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुशल के दुष्परिणामों का विशद विवेचन किया गया है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहां हुआ था?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ई मैं बस्ती जिले के आगोरा नामक गांव में हुआ था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के माता का नाम क्या था?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माता का नाम निवासी था।
जन्म - 4 अक्टूबर,1884 ई.
निधन - 2 फरवरी 1941 ई.
जन्म स्थान - बस्ती जिले के अगौना गांव में उत्तर प्रदेश
विधिवत शिक्षा इंटर तक हुई।
संस्कृत ,हिंदी ,अंग्रेजी का विषाद ज्ञान स्वाध्याय के बल पर प्राप्त किया।
पिता ने शुक्ल पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दिया पर वह आंख बचाकर हिंदी पढ़ते थे।
शुक्ला जी गणित में कमजोर थे
शुक्ला जी ने मिर्जापुर के पंडित केदार नाथ पाठक और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में आकर अध्ययन अध्यवसाय पर बल दिया।
1910ई. से 1910 ई. के लगभग हिंदी शब्द सागर के संपादन में वैतनिक सहायक के रूप में काशी रहे।
शुक्ला जी कुछ समय हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के हिंदी अध्यापक रहे।
शुक्ला जी ने महीने भर के लिए अलवर में भी नौकरी की।
विभागाध्यक्ष नियुक्ति हुई इसी पद पर रहते हुए 1941 ईस्वी में श्वास के दौरे में हृदय गति बंद होने से उनकी मृत्यु हुई।
शुक्ल जी द्वारा संपादित कृतियां
जायसी ग्रंथावली (1925 ईस्वी)
भ्रमरगीत सार (1926 ईस्वी)
गोस्वामी तुलसीदास
वीर सिंह देव चरित
भारतेंदु संग्रह
हिंदी शब्द सागर
मौलिक रचना - कविताएं
जायसी
तुलसी
सूरदास
रस मीमांसा (1949 ईस्वी)
भारत में वसंत
मनोहारी छटा
मधु स्रोत
अनुवाद कार्य
कल्पना का आनंद
राज्य प्रबंध शिक्षा
विश्व प्रपंच
आदर्श जीवन
मेगस्थनीज का भारत विषय का वर्णन
बुद्ध चरित्र
शशांक
हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 (ईसवी)
फारस का प्राचीन इतिहास
निबंध संग्रह
काव्य में रहस्यवाद (1929 ईस्वी)
विचार वीथी 1930 (ईस्वी), 1912 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक
रस मीमांसा (1949 ईस्वी)
चिंतामणि भाग 1 (1945 ईस्वी)
चिंतामणि भाग 2 (1945 ईस्वी)
चिंतामणि भाग 3 (नामवर सिंह द्वारा संपादित)
चिंतामणि भाग 4 (कुसुम चतुर्वेदी संपादित शुक्ल द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकों की भूमिका और गोष्ठियों में दिए गए उदाहरण।)
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध
काव्य में प्राकृति दृश्य
रसात्मक बोध के विविध स्वरूप
काव्य में अभिव्यंजनावाद
कविता क्या है?
काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था
भारतेंदु हरिश्चंद्र
काव्य में रहस्यवाद
मानस की जन्मभूमि
साहित्य
उपन्यास
मित्रता
साधारणीकरण और व्यक्ति
तुलसी का भक्ति मार्ग
करुणा निबंध का सारांश लिखिए ?
सारांश यह है कि कवना के प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में परोपकार की भावना का मूल तत्व करुणा ही है। बुधवा महावीर ने करुणा पर अत्यधिक बल दिया है। कहा से मिलता जुलता एक अन्य भाव दया है। दया वा कुंडा में निम्नलिखित अंतर है।
दया करुणा में अंतर -
दया एक विशिष्ट भाव है जो किसी विशिष्ट प्राणी या व्यक्ति के प्रति उत्पन्न होती है, जैसे विशेष परिस्थिति में सड़क पर किसी दुर्घटना ग्रस्त जीव को देखकर दया का भाव आना। इसके विपरीत करुणा विशिष्ट के प्रति ही नहीं सामान के प्रति भी हो सकती है। बुद्ध ने करुणा को नैतिकता का मूल आधार माना है और वह करुणा सामान्य के प्रति ही है।
दया में यह निहित तो होता है कि दया का पात्र खुद उबरने में समर्थ नहीं है जबकि दया करने वाला सामर्थ्य हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए राम श्याम से अधिक ताकतवर है और उसे मार रहा है और श्याम उससे दया की भीख मांगे तो राम समर्थ है दूसरी ओर यदि राम की दुर्घटना किसी बात से हो जाती है और चोट ऐसी है कि कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सकता तो ऐसे समय डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति दया का भाव रखेगा तो भी असमर्थ ही होगा इसके विपरीत करुणा के लिए यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति अपनी स्थिति से बाहर निकलने में अक्षम हो।
दया एक तत्कालीन मानसिक अवस्था है इसके विपरीत करुणा तुलनात्मक रूप से स्थाई भाव है।
शुक्ला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया ?
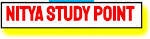
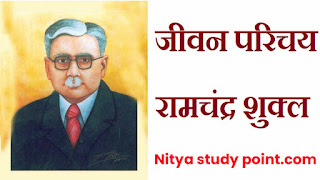

Post a Comment