भाषा किसे कहते हैं? - Bhasha kise kahate Hain. परिभाषा ,उदाहरण, प्रकार एवं भेद
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका Nitya study point.com के एक नए आर्टिकल में इस आर्टिकल में पढ़ेंगे की भाषा किसे कहते हैं? जिसके बाद हम हिंदी व्याकरण पड़ेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की तैयारी के लिए आप इस वेबसाइट को फॉलो करें ।
भाषा वह माध्यम है, जिसके द्वारा मानव बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि- जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके तथा दूसरों के भावो को समझ सके उसे भाषा कहते है।
सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि - सामान्यतः भाषा मानव की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते है।
डॉ श्याम सुन्दर दास के अनुसार परिभाषा - "मानव तथा मानव के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा तथा मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतो का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते है"।
डॉ बाबुराम सक्सेना के अनुसार परिभाषा -" जिन ध्वनि-चिंहों द्वारा मानव परस्पर विचार-बिनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते है"।
ऊपर दी गई परिभाषाओं से निम्नवत निष्कर्ष निकलते है-
(I) भाषा में ध्वनि-संकेतों का परम्परागत तथा रूढ़ प्रयोग होता है।
(II) भाषा के सार्थक ध्वनि-संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है।
(III) भाषा के ध्वनि-संकेत किसी समाज या वर्ग के आन्तरिक तथा ब्राह्य कार्यों के संचालन या विचार-विनिमय में सहायक होते हैं।
(IV) हर वर्ग या समाज के ध्वनि-संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भित्र होते हैं।
दोस्तों, आदिमानव अपने मन के भाव एक-दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदिमानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए तथा शब्दों के मेल से बनी- भाषा।
भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। जिसका तात्पर्य है- बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं तथा छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता-पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है तथा वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार, छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं तथा अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान-प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु-पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता।
इसके द्वारा मानव के भावो, विचारो तथा भावनाओ को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषावैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है। किन्तु ये परिभाषा पूर्ण नही है। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पायी जाती है।
आचार्य देवनार्थ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनायी है। उच्चरित ध्वनि संकेतो की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मानव परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते है उस यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते है।
यहाँ तीन बातें विचारणीय है- (I) भाषा ध्वनि संकेत है; (II) वह यादृच्छिक है; (III) वह रूढ़ है।
(i) सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते है। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मानव के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है; किन्तु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झण्डी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलनेवाली है; किन्तु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्त्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक-ठीक समझ भी नहीं पाते तथा न इनसे विचार ही सही-सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक तथा स्पष्ट होना चाहिए।
(ii) भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द तथा अर्थ में कोई तर्क-संगत सम्बन्ध नहीं रहता। बिल्ली, कौआ, घोड़ा, आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है।
(iii) भाषा के ध्वनि-संकेत रूढ़ होते हैं। परम्परा या युगों से इनके प्रयोग होते आये हैं। तथात, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनन्तकाल से करते आ रहे है। बच्चे, जवान, बूढ़े- सभी इनका प्रयोग करते है। क्यों करते है, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन हैं।
भाषा व्यक्त करने के चाहे जो भी तरीके हों, हम किसी-न-किसी शब्द, शब्द-समूहों या भावों की ओर ही इशारा करते हैं जिनसे सामनेवाले अवगत होता है। इसलिए भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों की बातें करते हैं। इन शब्दों या शब्द-समूहों (वाक्यों) द्वारा हम अपनी आवश्यकताएँ, इच्छाएँ, प्रसन्नता या खिन्नता, प्रेम या घृणा, क्रोध अथवा संतोष प्रकट करते हैं। हम शब्दों का प्रयोग कर बड़े-बड़े काम कर जाते हैं या मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर बने-बनाए काम को बिगाड़ बैठते हैं।
हम इसके प्रयोग कर किसी क्रोधी के क्रोध का शमन कर जाते हैं तो किसी शांत-गंभीर व्यक्ति को उत्तेजित कर बैठते हैं। किसी को प्रोत्साहित तो किसी को हतोत्साहित भी हम शब्द-प्रयोग से ही करते हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि हम भाषा के द्वारा बहुत सारे कार्यो को करते हैं। हमारी सफलता या असफलता (अभिव्यक्ति के अर्थ में) हमारी भाषायी क्षमता पर निर्भर करती है।
भाषा से हमारी योग्यता-अयोग्यता सिद्ध होती है। जहाँ अच्छी तथा सुललित भाषा हमें सम्मान दिलाती है वहीं अशुद्ध तथा फूहड़ भाषा हमें अपमानित कर जाती है (समाज में) । स्पष्ट है कि भाषा ही मानव की वास्तविक योग्यता, विद्वत्ता तथा बुद्धिमता, उसके अनुशीलन, मनन तथा विचारों की गंभीरता उसके गूढ़ उद्देश्य तथा उसके स्वभाव, सामाजिक स्थिति का परिचय देती है।
कोई अपमानित होना नहीं चाहता। इसीलिए, हमें हमेशा सुन्दर तथा प्रभावकारिणी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारा प्रयास लगातार जारी रहे। भाषा में पैठ एवं अच्छी जानकारी के लिए हमें निम्नवत बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए-
(1) हम छोटी-छोटी भूलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखें तथा उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। चाहे जहाँ कहीं भी हों अपनी भाषायी सीमा का विस्तार करें। दूसरों की भाषा पर भी ध्यान दें।
(2) खासकर बच्चों की भाषा पर विशेष ध्यान दें। यदि हम उनकी भाषा को शुरू से ही व्यवस्थित रूप देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उसका (भाषा का) वातावरण तैयार होगा।
(3) सदा अच्छी व ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों का अध्ययन करें। उन पुस्तकों में लिखे नये शब्दों के अर्थों एवं प्रयोगों को सीखें। लिखने एवं बोलने की शैली सीखें।
(4) वाक्य-प्रयोग करते समय इस छोटी-सी बात का हमेशा ध्यान रखें-
हर संज्ञा के लिए एक उपयुक्त विशेषण एवं प्रत्येक क्रिया के लिए सटीक क्रिया-विशेषण का प्रयोग हो।
(5) विराम-चिह्नों का प्रयोग उपयुक्त जगहों पर हो। लिखते तथा बोलते समय भी इस बात का ध्यान रहे।
(6) मुहावरे, लोकोक्तियों, बिम्बों आदि का प्रयोग करना सीखें तथा आस-पास के लोगों को सिखाएँ।
(7) जिस भाषा में हम अधिक जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, हमें उसके व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है।
हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा परिवर्तनशील होती है। किसी भाषा में नित नये शब्दों, वाक्यों का आगमन होते रहता है तथा पुराने शब्द टूटते, मिटते रहते हैं। किसी शब्द या वाक्य को पकड़े रहना कि यह ऐसा ही प्रयोग होता आया है तथा आगे भी ऐसा ही रहेगा या यही रहेगा- कहना भूल है। आज विश्व में कुल 2,796 भाषाएँ तथा 400 लिपियाँ मान्यता प्राप्त हैं। एक ही साथ इतनी भाषाएँ तथा लिपियाँ नहीं आई। इनका जन्म विकास के क्रम में हुआ, टूटने-फूटने से हुआ।
हम जानते हैं कि हर भाषा का अपना प्रभाव हुआ करता है। हर आदमी की अपने-अपने हिसाब से भाषा पर पकड़ होती है तथा उसी के अनुसार वह एक-दूसरे पर प्रभाव डालता है। जब पारस्परिक सम्पर्क के कारण एक जाति की भाषा का दूसरी जाति की भाषा पर असर पड़ता है, तब निश्चित रूप से शब्दों का आदान-प्रदान भी होता है। यही कारण है कि कोई भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह पाती तथा उससे अनेक शाखाएँ विभिन्न परिस्थितियों के कारण फूटती रहती हैं तथा अपना विस्तारकर अलग-अलग समृद्व भाषा का रूप ले लेती हैं। इस बात को हम एक सरल उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझने का प्रयास करें-
विचार कीजिए कि किसी कारण से अलग-अलग 5 भाषाओं के लोग कुछ दिन तक एक साथ रहे। वे अपनी-अपनी भाषाओं में एक-दूसरे से बातें करते-सुनते रहे। पांचों ने एक दूसरे की भाषा के शब्द ग्रहण किए तथा अपने-अपने साथ लेते गए। अब प्रश्न उठता है कि पांचों में से किसी की भाषा अपने मूल रूप में रह पायी ? इसी तरह यदि दो-चार पीढ़ियों तक उन पांचो के परिवारों का एक-साथ उठना-बैठना हो तो निश्चित रूप से विचार-विनिमय के लिए एक अलग ही किस्म की भाषा जन्म ले लेगी, जिसमें पांचो भाषाओं के शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग होगा। उस नई भाषा में उक्त पांचो भाषाओं के सरल तथा सहज उच्चरित होनेवाले शब्द ही प्रयुक्त होंगे वे भी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार तथा सरलतम रूपों में; क्योंकि जब कोई एक भाषाभाषी दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करता है तो वह सरल से सरलतम शब्दों का चयन करके भी उसे अपने अनुसार सहज बना लेता है। निम्नवत उदाहरणों से इसका अंदाजा लगाएँ-
मूल शब्द : विकास के क्रम में बने सरल से सरलतम रूप (विभिन्न भाषाओं में)
बाह्य : बाह > बाहर
मध्यम : मुझ
सप्तत्रिंशत : सैंतीस
मनस्कामना : मनोकामना
दक्षिण : दखिन > दाहिन > दहिन > दाहिना
परीक्षा : परिखा > परख
अग्नि : अग्नि > आग
कुमार (संस्कृत) : कुँवर
जायगाह (फारसी) : जगह
लीचू (चीनी) : लीची
ओपियम (यूनानी) : अफीम
लैन्टर्न (अंग्रेजी) : लालटेन
किसी भाषा के दो मुख्य आधार हुआ करते हैं-
(1) मानसिक आधार तथा
(2) भौतिक आधार
मानसिक आधार से आशय है, वे विचार या भाव, जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है तथा भौतिक आधार के जरिए श्रोता ग्रहण करता है। इसके सहारे भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ (वर्ण, अनुतान, स्वराघात आदि) तथा इनसे निकलनेवाले विचारों या भावों को ग्रहण किया जाता है। जैसे- 'फूल' शब्द का प्रयोग करनेवाला भी इसके अर्थ से अवगत होगा तथा जिसके सामने प्रयोग किया जा रहा (सुननेवाला) वह भी। यानी भौतिक आधार अभिव्यक्ति का साधन है तथा मानसिक आधार साध्य। दोनों के मिलने से ही भाषा का निर्माण होता है। इन्हें ही 'ब्राह्य भाषा' तथा आन्तरिक भाषा कहा जाता है।
भाषा समाज-द्वारा अर्जित सम्पत्ति है तथा उसका अर्जन मानव अनुकरण के सहारे समाज से करता है। यह अनुकरण यदि ठीक-ठाक हो तो मानव किसी शब्द को ठीक उसी प्रकार उच्चरित करेगा, परन्तु ऐसा होता नहीं है। वाक्य, अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप में समझकर किया जाता हैं। अनुकरण करने में प्रायः अनुकर्त्ता कुछ भाषिक तथ्यों को छोड़ देता है तथा कुछ को जोड़ लेता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, भाषा का अनुकरण कर रही होती है, तब ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ- भाषा के पाँचों क्षेत्रों में इसे छोड़ने तथा जोड़ने के कारण परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है। इस अनुकरण की अपूर्णनता के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं-
शारीरिक विभिन्नता, एकाग्रता की कमी, शैक्षिक स्तरों में अंतर का होना, उच्चारण में कठिनाई होना, भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव आदि।
ऊपर दिए गए प्रभावों के कारण अनुकरणात्मक विविधता के कुछ उदाहरण देखें-
तृष्णा -तिसना/टिसना शिक्षा - सिच्छा
षड्यंत्र - खडयंत्र रिपोर्ट -रपट
राजेन्द्र - रजिन्दर/राजेन्दर ट्रैजेडी -त्रासदी
अंदाज - अंजाद लखनऊ - नखलऊ
परीक्षा -परिच्छा क्षत्रिय - छत्री
स्टेशन -इस्टेशन/टिशन स्कूल - ईसकूल
प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्टभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाए है। जैसे- हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बँगला, गुजराती, उर्दू, तेलगु, कन्नड़, चीनी, आदि।
हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नवत लक्षण दिए है।
अनुकरण की यह प्रवृत्ति या भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। एक भाषा-क्षेत्र में कई बोलियाँ हुआ करती हैं तथा इसी तरह एक बोली-क्षेत्र में कई उपबोलियाँ। बोली के लिए विभाषा, उपभाषा अथवा प्रांतीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। बोली का क्षेत्र छोटा तथा भाषा का बड़ा होता है। यों तो प्रकृति की दृष्टि से भाषा तथा बोली में अन्तर कर पाना मुश्किल है फिर भी यहाँ कुछ सामान्य अन्तर दिए जा रहे हैं-
''बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है; किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलनेवाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलनेवालों के उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट तथा महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।''
भाषा का क्षेत्र व्यापक हुआ करता है। इसे सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएँ प्राप्त होती हैं; जबकि बोली को मात्र सामाजिक मान्यता ही मिल पाती है। भाषा का अपना गठित व्याकरण हुआ करता है; परन्तु बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। हाँ, बोली ही भाषा को नये-नये बिम्ब, प्रतीकात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि समर्पित करती है। जब कोई बोली विकास करते-करते उक्त सभी मान्यताएँ प्राप्त कर लेती है, तब वह बोली न रहकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे- खड़ी बोली हिन्दी जो पहले (द्विवेदी-युग से पूर्व) मात्र प्रांतीय भाषा या बोली मात्र थी वह आज भाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है।
एक बोली जब मानक भाषा बनती है तथा प्रतिनिधि हो जाती है तो आस-पास की बोलियों पर उसका भारी प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथली, मगही आदि सभी को प्रभावित किया है। हाँ, यह भी देखा जाता है कि कभी-कभी मानक भाषा कुछ बोलियों को बिल्कुल समाप्त भी कर देती है। एक बात तथा है, मानक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव ही देखा जाता है।
एक उदाहरण द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है-
बिहार राज्य के बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिलों में प्रायः ऐसा बोला जाता है-
हम कैह देंगे। हम नै करेंगे आदि।
भोजपुर क्षेत्र में : हमें लौक रहा है (दिखाई पड़ रहा है)। हम काम किये (हमने का) किया)
पंजाब प्रान्त का असर : हमने जाना है (हमको जाना है)
दिल्ली-आगरा क्षेत्र में : वह कहवे था/ मैं जाऊँ। मेरे को जाना है।
कानपुर आदि क्षेत्रों में : वह गया हैगा।
एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं, जबकि एक बोली में कई भाषाएँ नहीं होतीं। बोली बोलनेवाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली में बातें करते हैं; किन्तु बाहरी लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं।
ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा-परिवार, 179 भाषाएँ तथा 544 बोलियाँ हैं-
(a) भारोपीय परिवार : उत्तरी भारत में बोली जानेवाली भाषाएँ।
(b) द्रविड़ परिवार : तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम।
(c) आस्ट्रिक परिवार : संताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खड़िया, कोर्क, भूमिज, गदवा, पलौंक, वा, खासी, मोनख्मे, निकोबारी।
(d) तिब्बती-चीनी : लुशेइ, मेइथेइ, मारो, मिश्मी, अबोर-मिरी, अक।
(e) अवर्गीकृत : बुरूशास्की, अंडमानी
(f) करेन तथा मन : बर्मा की भाषा (जो अब स्वतंत्र है)
भाषा के प्रकार
भाषा के तीन (three) रूप होते है-
(i)मौखिक भाषा
(ii)लिखित भाषा
(iii)सांकेतिक भाषा।
(i)मौखिक भाषा :-विद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है।
इस प्रकार, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है।
दूसरे शब्दों में- जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दुसरो को समझाते है, उसे मौखिक भाषा कहते है।
जैसे: टेलीफ़ोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि।
मौखिक या उच्चरित भाषा, भाषा का बोल-चाल का रूप है। उच्चरित भाषा का इतिहास तो मानव के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मानव ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है।
यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मानव ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है।
मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-
(i) यह भाषा का अस्थायी रूप है।
(ii) उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है।
(iii) वक्ता तथा श्रोता एक-दूसरे के आमने-सामने हों प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।
(iv) इस रूप की आधारभूत इकाई 'ध्वनि' है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता हैं।
(v) यह भाषा का मूल या प्रधान रूप हैं।
(II) लिखित भाषा :-मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता-पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता-पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है।
इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है।
दूसरे शब्दों में- जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारो को लिखकर प्रकट करते है, उसे लिखित भाषा कहते है।
जैसे:पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार-पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि।
उच्चरित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। मानव को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचा दे तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता हुई होगी। अतः मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करने हेतु उच्चरितध्वनि प्रतीकों के लिए 'लिखित-चिह्नों' का विकास हुआ होगा।
इस तरह विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों ने अपनी-अपनी भाषिक ध्वनियों के लिए तरह-तरह की आकृति वाले विभिन्न लिखित-चिह्नों का निर्माण किया तथा इन्हीं लिखित-चिह्नों को 'वर्ण' (letter) कहा गया। अतः जहाँ मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि (Phone) है तो वहीं लिखित भाषा की आधारभूत इकाई 'वर्ण' हैं।
लिखित भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-
(i) यह भाषा का स्थायी रूप है।
(ii) इस रूप में हम अपने भावों तथा विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
(iii) यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता तथा श्रोता आमने-सामने हों।
(iv) इस रूप की आधारभूत इकाई 'वर्ण' हैं जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त (represent) करते हैं।
(v) यह भाषा का गौण रूप है।
इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है। किसी व्यक्ति को यदि लिखना-पढ़ना (लिखित भाषा रूप) नहीं आता तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उसे वह भाषा नहीं आती। किसी व्यक्ति को कोई भाषा आती है, इसका अर्थ है- वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात संप्रेषित कर लेता है।
(III) सांकेतिक भाषा :- जिन संकेतो के द्वारा बच्चे या गूँगे अपनी बात दूसरों को समझाते है, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है।
दूसरे शब्दों में- जब संकेतों (इशारों) द्वारा बात समझाई तथा समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है।
जैसे- चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक-बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि।
इसका अध्ययन व्याकरण में न
भाषा का उद्देश्य
भाषा का उद्देश्य है- संप्रेषण या विचारों का आदान-प्रदान।
भाषा के उपयोग ( Uses of Language)
भाषा विचारों के आदान-प्रदान का सर्वाधिक उपयोगी साधन है। परस्पर बातचीत लेकर मानव-समाज की सभी गतिविधियों में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। संकेतों से कही गई बात में भ्रांति की संभावना रहती है, किन्तु भाषा के द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट तथा निर्भ्रांत रूप में दूसरों तक पहुँचा सकते हैं।
भाषा का लिखित रूप भी कम उपयोगी नहीं। पत्र, पुस्तक, समाचार-पत्र आदि का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। लिखित रूप में होने से पुस्तकें, दस्तावेज आदि लम्बे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ तथा ऐतिहासिक शिलालेख आज तक इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वे भाषा के लिखित रूप में है।
भाषा की प्रकृति ( Nature of Language)
भाषा सागर की तरह सदा चलती-बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण-अवगुण होते है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है, जो मानव को प्राप्त होती है। मानव उसे अपने पूवर्जो से सीखता है तथा उसका विकास करता है।
यह परम्परागत तथा अर्जित दोनों है। जीवन्त भाषा 'बहता नीर' की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप है- कथित तथा लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा, या बोलकर तथा लेखन के द्वारा (लिखकर) करते हैं। देश तथा काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बँटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से तथा शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द तथा मूल ध्वनियाँ ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग-प्रत्यंगों का अध्ययन-विवेचन होता है। अतएव, व्याकरण भाषा पर आश्रित है।
भाषा के विविध रूप
(Various forms of Language)
हर देश में भाषा के तीन रूप मिलते है-
(1) बोलियाँ (2) परिनिष्ठित भाषा (3) राष्ट्र्भाषा
(1) बोलियाँ :- जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली कहते है।
किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास-पात की तरह अपने-आप जन्म लेती है तथा किसी क्षेत्र-विशेष में बोली जाती है। जैसे- भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलगु, इंग्लिश आदि।
(2) परिनिष्ठित भाषा :- यह व्याकरण से नियन्त्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन तथा साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ीबोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गयी है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्टभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लाँघकर अधिक व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र में विचार-विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में पन्द्रह विकसित भाषाएँ है, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' (राजभाषा) का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार, हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है- रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी आदि।
(3) राष्ट्र्भाषा :- जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है, तो वह राष्टभाषा बन जाती है।
दूसरे शब्दों में- वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है।
सभी देशों की अपनी-अपनी राष्ट्रभाषा होती है; जैसे- अमरीका-अंग्रेजी, चीन-चीनी, जापान-जापानी, रूस-रूसी आदि।
भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70-75 प्रतिशत लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है।
भाषा तथा लिपि
(Language & Script )
लिपि- शब्द का अर्थ है-'लीपना' या 'पोतना' विचारो का लीपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है।
दूसरे शब्दों में- भाषा की उच्चरित/मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिह्नों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं।
हिंदी तथा संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है।
मौखिक या उच्चरित भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चरित ध्वनि के लिए लिखित चिह्न या वर्ण बनाए गए। वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। वस्तुतः लिपि उच्चरित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है।
सभ्यता के विकास के साथ-साथ अपने भावों तथा विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, दूर-सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए तथा संदेशों तथा समाचारों के आदान-प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा से काम न चल पाया होगा तब मौखिक ध्वनि संकेतों (प्रतीकों) को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी होगी।
अनेक लिपियाँ :(Many Scripts)
किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है तो दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है या एक से अधिक भाषाओं को किसी एक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को हम देवनागरी तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं-
देवनागरी लिपि - राहुल बाजार गया है।
रोमन लिपि - Rahul bajar gaya hai.
इसके विपरीत हिंदी, मराठी, नेपाली, बोडो तथा संस्कृत सभी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं।
हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम 'देवनागरी लिपि' है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी की देवनागरी का ही नहीं गुजराती, बँगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है।
देवनागरी लिपि में बायीं ओर से दायीं ओर लिखा जाता है। यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एक मात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था है। संसार की समस्त भाषाओं में व्यंजनों का स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है पर देवनागरी के अलावा विश्व में कोई भी ऐसी लिपि नहीं है जिसमें व्यंजन तथा स्वर को मिलाकर लिखे जाने की व्यवस्था हो। यही कारण है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि है।
अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियाँ बायीं ओर से दायीं ओर ही लिखी जाती हैं। केवल उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी जाती है दायीं ओर से बायीं ओर लिखी जाती है।
नीचे की तालिका में विश्व की कुछ भाषाओं तथा उनकी लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं-
क्रम भाषा लिपियाँ
1 हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो देवनागरी
2 अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटेलियन, पोलिश, मीजो रोमन
3 पंजाबी गुरुमुखी
4 उर्दू, अरबी, फारसी फारसी
5 रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानियन रूसी
6 बँगला बँगला
7 उड़िया उड़िया
8 असमिया असमिया
हिन्दी में लिपि चिह्न
(Script symbols in Hindi)
देवनागरी के वर्णो में 11 स्वर तथा 41 व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है, उसे मात्रा कहते हैं; जैसे-
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ
क का कि की कु कू के कै को कौ
देवनागरी लिपि
(Devnagari Script )
देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। 'हिन्दी' तथा 'संस्कृत' देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। 'देवनागरी' लिपि का विकास 'ब्राही लिपि' से हुआ, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। 8वीं एवं 9वीं सदी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों तथा बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने देशों में इसका प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में इसे 'बालबोध' के नाम से संबोधित किया गया।
विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे-सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल, शारदा तथा प्राचीन देवनागरी के रूप में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुँचा है। प्राचीन नागरी के दो रूप विकसित हुए- पश्चिमी तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों से विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ-
प्राचीन देवनागरी लिपि:
पश्चिमी प्राचीन देवनागरी- गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, नागरी
पूर्वी प्राचीन देवनागरी- कैथी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बँगला, असमिया
संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकासक्रम को निम्नवत आरेख से समझा जा सकता है-
ब्राह्मी:
उत्तरी शैली- गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि
प्राचीन नागरी लिपि:
पूर्वी नागरी- मैथली, कैथी, नेवारी, बँगला, असमिया आदि।
पश्चिमी नागरी- गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी, नागरी या देवनागरी।
दक्षिणी शैली-
देवनागरी लिपि पर तीन भाषाओं का बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
(i) फारसी प्रभाव : पहले देवनागरी लिपि में जिह्वामूलीय ध्वनियों को अंकित करने के चिह्न नहीं थे, जो बाद में फारसी से प्रभावित होकर विकसित हुए- क. ख. ग. ज. फ।
(ii) बांग्ला-प्रभाव : गोल-गोल लिखने की परम्परा बांग्ला लिपि के प्रभाव के कारण शुरू हुई।
(iii) रोमन-प्रभाव : इससे प्रभावित हो विभिन्न विराम-चिह्नों, जैसे- अल्प विराम, अर्द्ध विराम, प्रश्नसूचक चिह्न, विस्मयसूचक चिह्न, उद्धरण चिह्न एवं पूर्ण विराम में 'खड़ी पाई' की जगह 'बिन्दु' (Point) का प्रयोग होने लगा।
देवनागरी लिपि की विशेषताएँ
(Characteristics of Devnagari Script )
देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
(i) आ (ा), ई (ी), ओ (ो) तथा औ (ौ) की मात्राएँ व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं (जैसे- का, की, को, कौ); इ (ि) की मात्रा व्यंजन के पहले, ए (े) तथा ऐ (ै) की मात्राएँ व्यंजन के ऊपर तथा उ (ु), ऊ (ू),
ऋ (ृ) मात्राएँ नीचे लगायी जाती हैं।
(ii) 'र' व्यंजन में 'उ' तथा 'ऊ' मात्राएँ अन्य व्यंजनों की तरह न लगायी जाकर इस तरह लगायी जाती हैं-
र् +उ =रु । र् +ऊ =रू ।
(iii)अनुस्वार (ां) तथा विसर्ग (:) क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं;
जैसे- अ+ां =अं। क्+अं =कं। अ+:=अः। क्+अः=कः।
(iv) स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्गसहित एक व्यंजन वर्ण में बारह रूप होते हैं। इन्हें परम्परा के अनुस्वार 'बारहखड़ी' कहते हैं।
जैसे- क का कि की कु कू के कै को कौ कं कः।
व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं- खड़ी पाई के साथ तथा बिना खड़ी पाई के।
(v) ङ छ ट ठ ड ढ द र बिना खड़ी पाईवाले व्यंजन हैं तथा शेष व्यंजन (जैसे- क, ख, ग, घ, च इत्यादि) खड़ी पाईवाले व्यंजन हैं। सामान्यतः सभी वर्णो के सिरे पर एक-एक आड़ी रेखा रहती है, जो ध, झ तथा भ में कुछ तोड़ दी गयी है।
(vi) जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता, तब दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं।
जैसे- क्+त् =क्त । त्+य् =त्य । क्+ल् =क्ल ।
(vii) जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है, तब उसे 'द्वित्व व्यंजन' कहते हैं।
जैसे- क्क (चक्का), त्त (पत्ता), त्र (गत्रा), म्म (सम्मान) आदि।
(viii) वर्गों की अंतिम ध्वनियाँ नासिक्य हैं।
(ix) ह्रस्व एवं दीर्घ में स्वर बँटे हैं।
(x) उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है।
(xi) प्रत्येक वर्ग में अघोष फिर सघोष वर्ण हैं।
(xii) छपाई एवं लिखाई दोनों समान हैं।
(xiii) निश्चित मात्राएँ हैं।
(xiv) प्रत्येक के लिए अलग लिपि चिह्न है।
(xv) इसके ध्वनिक्रम पूर्णतया वैज्ञानिक हैं।
मातृभाषा
मातृभाषा- नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म पंजाबीभाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। राकेश पांडे का जन्म हिंदीभाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषाएँ हैं।
इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है, मातृभाषा कहलाती है।
दूसरे शब्दों में- बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है। यही 'मातृभाषा' कहलाती है।
प्रादेशिक भाषा
प्रादेशिक भाषा- जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे 'प्रादेशिक भाषा' कहते हैं।
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा- जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे- अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है।
राजभाषा
राजभाषा- वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राज-काज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है।
जैसे- भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों हैं। अमरीका की राजभाषा अंग्रेजी है।
मानक भाषा
मानक भाषा-विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है।
भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है; जैसे-
गयी - गई (मानक रूप)
ठण्ड - ठंड (मानक रूप)
अन्त - अंत (मानक रूप)
रव - ख (मानक रूप)
शुद्ध - शुदध (मानक रूप)
हिन्दी भाषा
(Hindi Language)
बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हिन्दी भाषा संस्कृत से निष्पन्न है; परन्तु यह बात सत्य नहीं है। हिन्दी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से हुई है तथा अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृत से। प्राकृत भाषा अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है। स्पष्ट है कि हमारे आदिम आर्यों की भाषा पुरानी संस्कृत थी। उनके नमूने ऋग्वेद में दिखते हैं। उसका विकास होते-होते कई प्रकार की प्राकृत भाषाएँ पैदा हुई। हमारी विशुद्ध संस्कृत किसी पुरानी प्राकृत से ही परिमार्जित हुई है। प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रशों तथा शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है।
हिन्दी भाषा तथा उसका साहित्य किसी एक विभाग तथा उसके साहित्य के विकसित रूप नहीं हैं; वे अनेक विभाषाओं तथा उनके साहित्यों की समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बहुत बड़े क्षेत्र- जिसे चिरकाल से मध्यदेश कहा जाता रहा है- की अनेक बोलियों के ताने-बाने से बुनी यही एक ऐसी आधुनिक भाषा है, जिसने अनजाने तथा अनौपचारिक रीति से देश की ऐसी व्यापक भाषा बनने का प्रयास किया था, जैसी संस्कृत रहती चली आई थी; किन्तु जिसे किसी नवीन भाषा के लिए अपना स्थान तो रिक्त करना ही था।
वर्तमान हिन्दी भाषा का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक हो चला। है इसे निम्नवत विभागों में बाँटा गया हैं-
(1) बिहारी भाषा (Bihari Language) : बिहारी भाषा बँगला भाषा से अधिक संबंध रखती है। यह पूर्वी उपशाखा के अंतर्गत है तथा बँगला, उड़िया तथा आसामी की बहन लगती है। इसके अंतर्गत निम्न बोलियाँ हैं- मैथली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी आदि। मैथली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ठाकुर तथा भोजपुरी के बहुत बड़े प्रचारक भिखारी ठाकुर हुए।
(2) पूर्वी हिन्दी (Eastern Hindi) : अर्द्धमागधी प्राकृत के अप्रभ्रंश से पूर्वी हिन्दी निकली है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों की रचना पूर्वी हिन्दी में ही की। दूसरी तीन बोलियाँ हैं- अवध, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचनाएँ इसी भाषा में लिखी हैं।
(3) पश्चिमी हिन्दी (Western Hindi) : पूर्वी हिन्दी तो बाहरी तथा भीतरी दोनों शाखाओं की भाषाओं के मेल से बनी हैं; परन्तु पश्चिमी हिन्दी का संबंध भीतरी शाखा से है।
यह राजस्थानी, गुजराती तथा पंजाबी से संबंध रखती है। इस भाषा के कई भेद हैं- हिन्दुस्तानी, ब्रज, कनौजी, बुँदेली, बाँगरू तथा दक्षिणी।
गंगा-यमुना के बीच मध्यवर्ती प्रान्त में तथा दक्षिण दिल्ली से इटावे तक ब्रजभाषा बोली जाती है। गुड़गाँव तथा भरतपुर, करोली तथा ग्वालियर तक ब्रजभाषी हैं। इस भाषा के कवियों में सूरदास तथा बिहारीलाल ज्यादा चर्चित हुए।
कन्नौजी, ब्रजभाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इटावा से इलाहाबाद तक इसके बोलनेवाले हैं। अवध के हरदोई तथा उन्नाव में यही भाषा बोली जाती है।
बुँदेली बुंदेलखंड की बोली है। झाँसी, जालौन, हमीरपुर तथा ग्वालियर के पूर्वी प्रान्त, मध्य प्रदेश के दमोह छत्तीसगढ़ के रायपुर, सिउनी, नरसिंहपुर आदि स्थानों की बोली बुँदेली है। छिंदवाड़ा तथा हुशंगाबाद के कुछ हिस्सों में भी इसका प्रचार है।
हिसार, झींद, रोहतक, करनाल आदि जिलों में बाँगरू भाषा बोली जाती है। दिल्ली के आसपास की भी यही भाषा है।
दक्षिण के मुसलमान जो हिन्दी बोलते हैं उसका नाम दक्षिणी हिन्दी है। इसके बोलनेवाले मुंबई, बरोदा, बरार, मध्य प्रदेश, कोचीन, कुग, हैदराबाद, चेन्नई, माइसोर तथा ट्रावनकोर तक फैले हैं। इन क्षेत्रों के लोग मुझे या मुझको की जगह 'मेरे को' बोलते हैं।
हिन्दुस्तानी भाषा के 2 रूप हैं। एक तो वह जो पश्चिमी हिन्दी की शाखा है, दूसरी वह जो साहित्य में काम आती है। पहली गंगा-यमुना के बीच का जो भाग है उसके उत्तर में रुहेलखंड में तथा अम्बाला जिले के पूर्व में बोली जाती है। यह पश्चिमी हिन्दी की शाखा है। यही धीरे-धीरे पंजाबी में परिणत हुई। मेरठ के आस-पास तथा उसके कुछ उत्तर में यह भाषा अपने विशुद्ध रूप में बोली जाती है। वहाँ उसका वही रूप है, जिसके अनुसार हिन्दी का व्याकरण बना है। रुहेलखंड में यह धीरे-धीरे कन्नौजी में तथा अंबाले में पंजाबी में परिणत हो गई है। या हिन्दुस्तानी तथा कुछ नहीं, सिर्फ ऊपरी दोआब की स्वदेशी भाषा है। दिल्ली में मुसलमानों के सहयोग से हिन्दी भाषा का विकास बहुत बढ़ा।
आधुनिक समय में इस भाषा का प्रचार इतना बढ़ गया है कि कोई प्रान्त, सूबा या शहर ऐसा नहीं रह गया है जहाँ इसके बोलनेवाले न हों। बंगाली, मद्रासी, गुजराती, मराठी, नेपाली आदि भिन्न भाषाएँ हैं फिर भी ये भाषा-भाषी हिन्दी को समझ लेते हैं। इसका व्याकरण वैज्ञानिक है। इस भाषा में संस्कृत के अलावा फ्रेंच, जापानी, बर्मी, चीनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि अनेकानेक भाषाओं के शब्दों की भरमार है। अतएव, इस भाषा का फैलाव बहुत तेजी से हुआ है। यही कारण है कि आज यह राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है।
याद रखने योग्य तथ्य
(Points to be remember)
'राजस्थानी हिन्दी' का विकास 'अपभ्रंश' से हुआ।
'पश्चिमी हिन्दी' का विकास 'शौरसेनी' से हुआ।
'पूर्वी हिन्दी' का विकास 'अर्द्धमागधी' से हुआ।
'बिहारी हिन्दी' का विकास 'मागधी' से हुआ।
'पहाड़ी हिन्दी' का विकास 'खस' से हुआ।
उपन्यास और कहानी में अंतर
महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर
छायावादी युग किसे कहते हैं? तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं
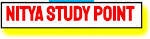


very help ful information sir ji
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteBhasha Kise Kahate Hain
ReplyDeletePost a Comment