जगन्नाथदास 'रत्नाकर' का जीवन परिचय || Jagannath Das Ratnakar ka Jivan Parichay
जीवन परिचय - जगन्नाथदास रत्नाकर का जन्म भाद्रपद सुदी 5, संवत् 1923 (सन् 1866 ईस्वी) को काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था। रत्नाकर जी के पिता पुरुषोत्तम दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे। वे फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता तथा हिंदी के परम प्रेमी थे।
रत्नाकर जी की शिक्षा का प्रारंभ उर्दू एवं फारसी भाषा के ज्ञान से हुआ। इन्होंने छठे वर्ष में हिंदी और आठवें वर्ष में अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात इन्होंने 'क्वींस कॉलेज बनारस' में प्रवेश लिया। सन् 1891 ईस्वी में इन्होंने बी.ए. की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात एम.ए. (फारसी) और एल.एल.बी. का अध्ययन प्रारंभ किया; किंतु अपनी माता जी के आकस्मिक निधन के कारण परीक्षा में सम्मिलित ना हो सके और इनकी शिक्षा का क्रम यहीं रुक गया।
सन 1900 ई० में रत्नाकर जी की नियुक्ति आवागढ़ (एटा) में कोषागार निरीक्षक के रूप में हुई। 2 वर्ष पश्चात रत्नाकर जी वहां से त्यागपत्र देकर चले आए तथा सन् 1902 ई० में अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के निजी सचिव नियुक्त हुए। अयोध्या नरेश की मृत्यु के बाद रत्नाकर जी महारानी के निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे और सन् 1928 ईस्वी तक इसी पद पर आसीन रहे। संवत् 1989 (सन् 1932 ईस्वी) में हरिद्वार में इनका निधन हो गया।
शिक्षा
जगन्नाथदास 'रत्नाकर' के रहन-सहन में राजसी ठाठ-बाट था। इन्हें हुक्का, इत्र, पान, घुड़सवारी आदि का बहुत शौक था। हिंदी का संस्कार उन्हें अपने हिंदी प्रेमी पिता से मिला था। स्कूली शिक्षा में उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। काशी के क्वींस कॉलेज से रत्नाकर जी ने सन् 1891 ई० में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें अंग्रेजी के साथ दूसरी भाषा फारसी भी थी। ये फारसी में m.a. की परीक्षा देना चाहते थे पर कुछ कारणों से ना दे सके।
जीविकोपार्जन
जगन्नाथ दास जी ने 'जकी' उपनाम से फारसी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया इस संबंध में इनके उस्ताद मोहम्मद हसन फायज थे। जब रत्नाकर जी जीविकोपार्जन की तरफ मुड़े तो वे अवागढ़ के खजाने के निरीक्षक नियुक्त हुए। सन 1902 में वे अयोध्या नरेश के निजी सचिव नियुक्त हुए, किंतु सन् 1906 में महाराजा का स्वर्गवास हो गया। लेकिन इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर महारानी जगदंबा देवी ने इन्हें अपना निजी सेक्रेटरी नियुक्त किया तथा मृत्युपर्यंत रत्नाकर जी इस पद पर रहे। अयोध्या में रहते हुए जगन्नाथदास रत्नाकर की कार्य-प्रतिभा समय-समय पर विकास के अवसर पाती रही। महारानी जगदंबा देवी की कृपा से उनकी काव्य कृति गंगावतरण सामने आई।
लेखनकार्य
जगन्नाथदास रत्नाकर हिंदी लेखन की ओर उस समय प्रवृत्त हुए, जब खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का व्यापक अभियान चल रहा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रीधर पाठक, पंडित नाथूराम शंकर शर्मा जैसे लोग खड़ी बोली हिंदी को भारी समर्थन दे रहे थे, लेकिन काव्य भाषा की बदलती लहर रत्नाकर जी के ब्रज भाषा प्रेम को अपदस्थ नहीं कर सकी। वे ब्रजभाषा का आंचल छोड़कर खड़ी बोली के पाले में जाने को किसी भी तरह तैयार नहीं हुए। जब उनके समकालीन खड़ी बोली के परिष्कार और परिमार्जन में सलंग्न थे, तब मैं ब्रजभाषा के त्रुटियों का परिष्कार कर साहित्यिक ब्रजभाषा के रूप के साथ संवार कर रहे थे। उन्होंने ब्रजभाषा का नए शब्दों, मुहावरों से ऐसा श्रंगार किया कि वे सूरदास, पद्माकर और घनानंद की ब्रजभाषा से अलग केवल उनकी ब्रजभाषा बन गई, जिसमें उर्दू और फारसी की रवानगी, संस्कृत का अभिजात्य और लोक भाषा की शक्ति समा गई। जिसके एक-एक वर्ण में एक-एक शब्द में और एक-एक पर्याय में भावलोक को चित्रित करने की अदम्य क्षमता है।
साहित्यिक परिचय - कविवर जगन्नाथ रत्नाकर आधुनिक युग के कवि थे। इनका आविर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हुआ था, परंतु इन्होंने आधुनिक युग की काव्य चेतना की उपेक्षा करके तथा मध्ययुगीन मनोवृति से प्रभावित होकर काव्य-साधना की तथा अपनी विलक्षण काव्यात्मक प्रतिभा से हिंदी काव्य जगत को प्रकाशित किया। रत्नाकर जी की काव्य-चेतना मध्ययुगीन मनोवृति से प्रभावित थी। मध्ययुगीन काव्य का विकास राज्याश्रय में हुआ था। रत्नाकर जी ने भी इसी प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया और सर्वप्रथम आवागढ़ के महाराजा तथा इसके पश्चात अयोध्या नरेश के निकट रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिया।
राज्याश्रय में अपनी काव्य-प्रतिभा का विकास करने के पश्चात भी रत्नाकर जी के काव्य में मात्र भावुकता एवं आश्रय दाताओं की प्रशस्ति ही नहीं है, वरन् इनके काव्य में व्यापक सह्रदयता का परिचय भी मिलता है। इनका काव्य-सौष्ठव एवं काव्य संगठन नूतन तथा मौलिक है। इन्हें काव्य के मर्म स्थलों की उत्कृष्ट पहचान थी और इन्होंने उसके भाव पक्ष के मर्म को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया। रत्नाकर जी के मुक्तकों में पौराणिक विषयों से लेकर देशभक्ति की आधुनिक भावनाओं तक को वाणी प्रदान की गई है।
कृतियां - रत्नाकर जी ने पद्म एवं गद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य-सर्जना की। वे मूलतः कवि थे, अतएव उनकी पद्य रचनाएं ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-
हिंडोला - यह सौ रोला छंदों का आध्यात्मपरक श्रृंगारिक निबंध काव्य है।
समालोचनादर्श - यह अंग्रेजी कवि पोप के समालोचना-संबंधित प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ 'Essay on Criticism' का हिंदी अनुवाद है।
हरिश्चंद्र - यह चार सर्गो का खंडकाव्य है, जो भारतेंदु जी के 'सत्य हरिश्चंद्र' नाटक पर आधारित है।
कलकाशी - यह 142 रोला छंदों का वर्णनात्मक प्रबंध-काव्य है, जो कि अपूर्ण है। यह प्रसिद्ध धार्मिक नगरी काशी से संबंधित है।
श्रंगार लहरी - इसमें श्रंगारपरक 168 कवित्त-सवैये हैं।
गंगा लहरी और विष्णु लहरी - यह दोनों रचनाएं 52-52 छंदों के भक्ति विषयक काव्य हैं।
रत्नाष्टक - इसमें देवताओं, महापुरुषों और षड्ऋतुओं से संबंधित 16 अष्टक संकलित हैं।
वीराष्टक - यह ऐतिहासिक वीरों और वीरांगनाओं से संबंधित 14 अष्टकों का संग्रह हैं।
प्रकीर्ण पद्यावली - इसमें फुटकर छंदों का संग्रह किया गया है।
गंगावतरण - यह गंगावतरण से संबंधित 13 सर्गों का आख्यानक प्रबंध-काव्य है।
उद्धव शतक - यह घनाक्षरी छंद में लिखित प्रबंध-मुक्तक दूत काव्य है।
इनके अतिरिक्त रत्नाकर जी ने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है, जिनके नाम हैं-सुधाकर, कविकुलकंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर-श्रृंगार, नखशिख, हम्मीर हठ, रस विनोद, समस्या पूर्ति, हिम-तरंगिणी, सुजान सागर, बिहारी-रत्नाकर तथा सूरसागर (अपूर्ण)।
रत्नाकर जी ने अनेक साहित्यिक और ऐतिहासिक लेख भी लिखें। उनके लिखित व्याख्यान भी हैं, जो बड़े ही गंभीर एवं विचारोत्तेजक हैं।
ऐतिहासिक लेख
शिवाजी का नया पत्र, शुगवंश का एक शिलालेख, एक प्राचीन मूर्ति घनाक्षरी निय रत्नाकर, समुद्रगुप्त का पाषाणश्व सवैया, छंद वर्ग इत्यादि।
सुधा सागर कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, हम्मीर हठ रसिक विनोद, समस्यापूर्ति, सुजानसागर,हिततरंगिणी।
काव्यगत विशेषताएं
(अ) भाव पक्ष
कविवर रत्नाकर भावों के कुशल चितेरे हैं। इन्होंने मानव हृदय के कोने-कोने को झांककर भावों के ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं कि उन्हें पढ़ते ही हृदय गद्गद हो उठता है।
रत्नाकर जी ने केवल श्रंगार रस का ही चित्रण नहीं किया, वरन् उनके काव्य में करुणा, उत्साह, क्रोध एवं घृणा आदि भावों का चित्रांकन भी बड़ी कुशलता से हुआ है।
रत्नाकर जी के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रत्नाकर जी के 'उद्धव शतक' में वियोग श्रृंगार की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनके काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों के भी दर्शन होते हैं।
(ब) कला पक्ष
भाषा - रत्नाकर जी पूर्ण कलाविद्, भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। इनकी भाषा प्रौढ साहित्यिक ब्रजभाषा है, परंतु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपनाकर इन्होंने अपनी भाषा का श्रंगार किया है। रत्नाकर जी ने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। श्रंगार के प्रसंग में भाषा की सरसता तथा वीरता के प्रसंग में भाषा का ओज काव्य-रसिकों का मन मोह लेता है। वे शब्द चित्र उतारने में पूर्णतया कुशल हैं। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा के चमत्कार और भाव-प्रेषण की शक्ति को द्धिगुणित कर दिया है।
शैली - रत्नाकर जी ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रण शैली, आलंकारिक शैली तथा चामत्कारिक शैली आदि का प्रयोग किया है।
रत्नाकर जी ने शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित अलंकारों के प्रयोग किए हैं। शब्द पर आधारित अलंकार तो स्वत: ही भाषा-प्रवाह के साथ आ गए हैं। अनुप्रासों का इतना सुंदर प्रयोग या तो रत्नाकर जी ने किया है या इस प्रकार का प्रयोग पद्माकर जी के काव्य में देखने को मिलता है।
रत्नाकर जी ने अनुप्रास के अतिरिक्त यमक, रूपक, वीप्सा, श्लेष, पुनरुक्तिप्रकाश, विभावना आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों में इनका सर्वप्रिय अलंकार सांगरूपक है। रत्नाकर जी सांगरूपकों के सम्राट हैं। 'उद्धव-शतक' के मंगलाचरण का प्रारंभ है सांगरूपक हुआ है-
जासौं जाति विषय-विषाद की बिवाई बेगि,
चोप चिकनाई चित्त चारू गहिबौ करै।
कहै 'रत्नाकर' कवित्त-वर-व्यंजन में,
जासौं स्वाद सौगुनी रुचिर रहिबौ करै।।
रत्नाकर जी ने अपने काव्य में प्रायः दो प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है-रोला तथा घनाक्षरी। इनके अतिरिक्त छप्पय,सवैया एवं दोहा आदि छंदों का प्रयोग भी यत्र-तत्र किया गया है। रत्नाकर जी का सर्वाधिक प्रिय छंद कवित्त है।
हिंदी साहित्य में स्थान - रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक हैं, जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व तथा अपनी मान्यताओं को इन्होंने अपने काव्य में सफल बाणी प्रदान की। इन्होंने नवीनता के आकर्षण में अपनी प्राचीन परंपरा को भुला देने की प्रवृत्ति के प्रति भावी पीढ़ी को सजग किया है। जिस परिस्थिति और वातावरण में इनका व्यक्तित्व गठित हुआ था, उसकी छाप इनकी साहित्यिक रचनाओं पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।
People Also Asked -
प्रश्न-जगन्नाथदास रत्नाकर का जन्म कब हुआ था?
उत्तर- जगन्नाथदास रत्नाकर का जन्म भाद्रपद सुदी 5, संवत् 1923 (सन् 1866 ईस्वी) को काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था।
प्रश्न-रत्नाकर का मतलब क्या होता है?
उत्तर-रत्नाकर नाम का मतलब रत्नों से मेरा सागर होता है।
प्रश्न-जगन्नाथदास रत्नाकर किस काल के कवि हैं?
उत्तर-रत्नाकर जी आधुनिक युग के ब्रज भाषा के कवि हैं।
प्रश्न-जगन्नाथदास रत्नाकर की मृत्यु कब हुई थी?
उत्तर- जगन्नाथदास रत्नाकर जी की मृत्यु संवत् 1989 (सन् 1932 ईस्वी) में हरिद्वार में हुई थी।
इन्हें भी पढ़ें 👉👉
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय
राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय
रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय
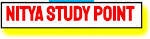


Post a Comment