कहानी और उपन्यास में अंतर | Kahani aur Upnyas Mein Antar
कहानी और उपन्यास में अंतर -
कहानी किसे कहते हैं?
कहानी - कहानी गद्य साहित्य का कोई नया रूप-विधान नहीं है। यह विधा जीवन के किसी एक संक्षिप्त प्रसंग की मार्मिक झलक दिखाने के उद्देश्य के साथ जन्मी और पर्याप्त विकसित हुई। 'एक क्षण में घनीभूत जीवन-दृश्य का अंकन' इसका उद्देश्य बन गया और जीवन के किसी मार्मिक क्षण में संवेदित होकर उसे कलात्मक एवं रोचक ढंग से रूपायित करना कहानीकार का कर्म बन गया। कहानी किसी मार्मिक घटना, मनोगत भावना, अनुभव या सत्य के चयन को अतिरंजन की कलात्मक रीति से संक्षेप में प्रतिबिम्बित करती है। इस प्रकार कहानी जीवन का खण्ड-चित्र है।
प्रसिद्ध समीक्षक बाबू श्यामसुन्दर दास ने कहानी को "एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर रचे गये नाटकीय आख्यान" की संज्ञा दी है। कहानीकार अज्ञेय की दृष्टि में "कहानी एक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र है, जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं।" इस प्रकार कहानी वह संक्षिप्त कथात्मक गद्य-विधा हैं, जिसमें जीवन की कोई एक भंगिमा या संवेदना या घटना झिलमिलाती हुई दीख पड़ती है। यह साहित्य का वह विकसित कलात्मक रूप है, जिसमें लेखक अपनी कल्पनाशीलता के सहारे कम-से-कम पात्रों अथवा चरित्रों के द्वारा कम-से-कम घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से अधिक-से-अधिक प्रभाव की सृष्टि करता है।
भारतेन्दु से पहले की हिन्दी कहानियों में इंशा अल्ला खाँ की 'रानी केतकी की कहानी' की विशेष चर्चा की जाती है। विद्वान् इसे हिन्दी की प्रथम कहानी मानते हैं, परन्तु कहानी कला की दृष्टि से इसे आधुनिक कहानी नहीं कहा जा सकता। भारतेन्दु युग में उत्कृष्ट कहानी सामने नहीं आयी । द्विवेदी युग में किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती'; बंग महिला की 'दुलाईवाली' और रामचन्द्र शुक्ल की 'ग्यारह वर्ष का समय' कहानियों को हिन्दी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। इनमें 'इन्दुमती' से ही कहानी का जन्म माना जाता है।
द्विवेदी युग के उत्तरार्द्ध में प्रसाद और प्रेमचन्द्र के आगमन के साथ ही हिन्दी कहानी के क्षेत्र में युगान्तर उपस्थित हुआ। प्रसाद जी की कहानियों में— 'आकाशदीप', 'पुरस्कार', 'ममता', 'मधुआ', 'चित्र- मन्दिर', 'गुण्डा' आदि प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी कहानियों में भाव, भाषा और कल्पना का पूर्ण उत्कर्ष दिखाते हुए मानव मन के अन्तर्द्वन्द्व का सजीव चित्रण किया है। इनके साथ ही प्रेमचन्द ने भी सरल व्यावहारिक भाषा-शैली में यथार्थ का मार्मिक चित्रण करने वाली आदर्शोन्मुखी कहानियों की रचना की। इनकी कहानियों में 'शतरंज के खिलाड़ी', 'कफन', 'पंच परमेश्वर', 'मन्त्र', 'ईदगाह' आदि प्रमुख हैं। इसी काल में। चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की 'उसने कहा था' कहानी लिखी गयी थी। इसे हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। इस युग के कहानीकारों में राधिकारमण सिंह, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', ज्वालादत्त शर्मा, विशम्भरनाथ जिज्जा और जी० पी० श्रीवास्तव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी की प्रारम्भिक कहानियाँ इसी काल में प्रकाशित हुई थीं। सन् 1935 ई० से हिन्दी कहानी एक नयी दिशा की ओर मुड़ी। इस युग में सामाजिक चेतना और यथार्थ जीवन को व्यक्त करने वाली कहानियों का श्रीगणेश हुआ तथा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी गयीं। इस युग के जैनेन्द्र कुमार हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक हैं। इन्होंने हिन्दी कहानी को एक नवीन अन्तर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की तथा हिन्दी कहानी के बौद्धिक स्तर को भी ऊँचा उठाया। इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय को जैनेन्द्र को मनोवैज्ञानिकता से प्रभावित कहानी-लेखक कहा जा सकता है। इन लेखकों में मनोविश्लेषण के प्रति इतना आग्रह है कि वे मानसिक रुग्णताओं को ही मानवीय सत्य मानकर अपने पात्रों के कृत्यों का यथातथ्य प्रकृतिवादी आकलन करते हैं। और भावना का ऐसा सामाजिक विद्रूप हिन्दी में अन्यत्र नहीं मिलता। इस युग के प्रमुख कहानीकार जैनेन्द्र कुमार, सियारामशरण गुप्त सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय', इलाचन्द्र जोशी, यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', रांगेय राघव, विष्णु प्रभाकर आदि है।
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् नयी कहानी का आगमन हुआ। इस युग की कहानियों में भाव-बोध और सौन्दर्य-बोध के नये द्वार खुले। वर्तमान युग में मानव जीवन की कुण्ठा, उलझन, दिशाहीनता, मानसिक भटकाव आदि का सूक्ष्म चित्रण इन कहानियों में नवीन शैली शिल्प के रूप में किया जा रहा है। इस युग के प्रसिद्ध कहानीकारों में फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, शैलेश मटियानी, शिवानी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, मन्नू भण्डारी, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, अमरकान्त, शिवप्रसाद सिंह, द्विजेन्द्रनाथ मिश्र 'निर्गुण' आदि है।
इसके अतिरिक्त अनेक कहानीकारों ने किसी आन्दोलन विशेष के साथ न जुड़कर भी अपने जीवन की व्यापक अनुभूतियों को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह सन्तोष की बात है कि हिन्दी कहानी अति यथार्थवाद, भोगवाद एवं उच्छृंखलतावाद के चक्रव्यूह से निकलकर व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन की ओर उन्मुख हुई है। इसीलिए आज की कहानियों में हम भारतीय गाँव,शहर और नगर के जीवन से सम्बन्धित विविध वर्गों का चित्रण सहज और स्वाभाविक रूप में देखते हैं, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक आदि सभी पक्षों का चित्रण न्यूनाधिक रूप में होता है। कहानी निश्चय ही दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। हमारा विश्वास है कि यदि इसकी स्थिति, दृष्टि एवं गति यही रही तो यह न केवल कला के उच्च आयामों का स्पर्श कर सकेगी, अपितु जीवन के लिए स्वस्थ, व्यापक एवं नये मूल्यों की भी प्रतिष्ठा कर सकेगी।
उपन्यास किसे कहते हैं?
उपन्यास - उपन्यास वर्तमान हिन्दी साहित्य की सर्वप्रिय और सशक्त विधा है। इसका कारण यह कि उपन्यास में मनोरंजन का तत्त्व तो निहित रहता ही है, साथ ही इसमें जीवन की बहुमुखी छवि को व्यक्त करने की क्षमता भी होती है। 'उपन्यास' शब्द का शाब्दिक अर्थ है- 'उप' – निकट या सामने, 'न्यास'-रखना, अर्थात् 'सामने रखना'। इसमें 'प्रसादन' अर्थात् प्रसन्न करने का भाव भी निहित है। अतः किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यस्त करना कहा जाएगा। किन्तु इस अर्थ में आजकल 'उपन्यास' का प्रयोग नहीं होता। हिन्दी में 'उपन्यास' को अंग्रेजी के 'नॉवेल' शब्द का पर्याय माना जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उपन्यास गद्य की वह विधा है; जिसमें जीवन का व्यापक चित्रण रोचक एवं सजीव शैली में किया गया हो। बाबू श्यामसुन्दर दास ने 'उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा' कहा है। उपन्यास का स्वरूप इतना शक्तिशाली है कि इसमें सहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित करने की क्षमता है। उपन्यास में कथा तो है ही, साथ ही अवसर आने पर यह काव्य की-सी भावुकता और संवेदना जगाकर पाठकों को तल्लीन करता है।
हिन्दी उपन्यासों की विकास-परम्परा को हम तीन भागों-पूर्व-प्रेमचन्द युग, प्रेमचन्द युग तथा प्रेमचन्दोत्तर युग में विभाजित करके इस परम्परा का अध्ययन करेंगे। प्रेमचन्द के नाम से इस विकास-परम्परा को विभाजित करने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। कि प्रेमचन्द जी अपने युग के ही नहीं वरन् सम्पूर्ण हिन्दी उपन्यास-साहित्य के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सर्जक रहे हैं। सन् 1882 ई० में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित 'परीक्षा गुरु' को हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। यह पूर्व-प्रेमचन्द युग की रचना है। इस युग के उपन्यासों में गम्भीरता का प्रायः अभाव है तथा ये घटनाप्रधान हैं। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं- बालकृष्ण भट्ट (नूतन ब्रह्मचारी); किशोरीलाल गोस्वामी (लवंगलता, कनक कुसुम, प्रणयिनी परिणय आदि); देवकीनन्दन खत्री (चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्ता सन्तति, भूतनाथ आदि); गोपालराम गहमरी (अद्भुत लाख, गुप्तचर आदि); ब्रजनन्दन सहाय (राजेन्द्र मालती, सौन्दर्योपासक आदि) आदि। इन उपन्यासों के साथ-साथ इस युग में बंगला उपन्यासों के सर्वाधिक अनुवाद हिन्दी में हुए। इसी युग के अन्तिम वर्षों में प्रेमचन्द जी 'रूठी रानी', 'प्रेमा' और 'सेवा सदन' । उपन्यासों की रचना कर चुके थे।
हिन्दी उपन्यासों के विकास में प्रेमचन्द का सर्वाधिक योगदान रहा है। प्रेमचन्द युग के उपन्यासों में सामाजिक जीवन और मानव चरित्र का विशद् चित्रण हुआ है। प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यास को सामयिक-सामाजिक जीवन से सम्बद्ध करके एक नया मोड़ दिया था। ये उपन्यास को 'मानव चरित्र का चित्र' समझते थे। इनकी दृष्टि से मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है। इस युग में प्रेमचन्द ने- 'निर्मला', 'गबन', 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि', 'गोदान': जयशंकर प्रसाद ने 'कंकाल', 'तितली', 'इरावती' (अपूर्ण) जैसे सशक्त उपन्यास हिन्दी को दिये। इनके अतिरिक्त इस युग के प्रमुख उपन्यासकार पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', भगवती प्रसाद वाजपेयी, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त भी इस युग में अनेक उपन्यासकार हुए। डॉ० विश्वनाथ तिवारी ने ठीक ही लिखा है कि "हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्द के आगमन से एक नवीन अध्याय प्रारम्भ होता है।"
प्रेमचन्द के पश्चात् उपन्यास-काल दो कालों में विभाजित हो गया - स्वतन्त्रता पूर्व और स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यास। इस युग सामाजिक उपन्यास अधिक लिखे गये। इन सभी उपन्यासों का लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना में और आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का सन्देश देना है। इस युग में जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी और अज्ञेय ने उपन्यास में मनोविज्ञान का विशेष समावेश किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी उपन्यास अनेक नयी दिशाओं में विकसित हुआ। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार हैं-जैनेन्द्र (परख, सुनीता, त्यागपत्र आदि); इलाचन्द्र जोशी (जहाज का पंछी, घृणापथ आदि); अज्ञेय (शेखर: एक जीवनी, नदी के द्वीप)। इस युग के अन्य उपन्यासकार हैं- यशपाल, रांगेय राघव, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', फणीश्वरनाथ रेणु, राहुल सांकृत्यायन, हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि।
साठोत्तर वर्षों में हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में जो मोड़ आया, उसमें मध्यम वर्ग की गाथा तो है ही, जीवन के प्रति तीखापन और कटुता का विष भी व्यक्त होता है। इस युग के उपन्यासों में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को महत्ता प्राप्त हुई तथा कथाहीनता व कथायुक्तता दोनों की प्रवृत्तियाँ भी साथ-साथ विकसित होती रहीं। इनके साथ ही प्राचीन कथाएँ भी पुनः संशोधित होकर अथवा समकालीन सन्दर्भों में विश्लेषित होकर श्रेष्ठ उपन्यासों के रूप में सामने आयीं। इस काल के प्रमुख उपन्यासकार हैं-हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्रीलाल शुक्ल, नरेन्द्र कोहली, 'अज्ञेय', निर्मल वर्मा, अमृतराय, विष्णु प्रभाकर, शिवानी, शैलेश मटियानी, नागार्जुन, कमलेश्वर, डॉ० देवराज, डॉ० राही मासूम रजा आदि ।
समग्रतः हम कह सकते हैं कि उपन्यास आज के गद्य लेखक की केन्द्रीय विधा हो चली है तथा इसका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। वस्तुत: उपन्यास गद्य साहित्य की वह महत्त्वपूर्ण विधा है, जो मनुष्य को उसकी समग्रता में व्यक्त करने में समर्थ है। हिन्दी उपन्यास का सौ वर्षों का इतिहास उसके द्रुत विकास और उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है।
जीवनी और आत्मकथा में अंतर
महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर
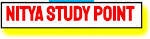

Post a Comment