Class 11th sociology varshik paper 2023 MP Board || एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं समाजशास्त्र वार्षिक पेपर 2023
[2211102-A]
समाजशास्त्र sociology
समय-3 घंटे पूर्णांक-100
निर्देश :-
(1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
(2) प्रश्नों के उत्तर सटीक होने चाहिए।
(3) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है।
(4) वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प दिये गये है।
(5) प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक के लिए 4 अंक निर्धारित है।
( 6 ) प्रश्न क्रमांक 13 से 19 तक के लिए 5 अंक निर्धारित है।
(7) प्रश्न क्रमांक 20 से 21 के लिए 6 अंक निर्धारित है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न-
प्रश्न 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
i) समाज शास्त्र का जनक…... कहा जाता है।
उत्तर- आंगस्त कांम्ट
ii) समाज…….. है ।
उत्तर- अमूर्त
iii) प्राथमिक समूह आकार में बहुत……... होते है।
उत्तर- छोटे
iv) पद्धति वह व्यवस्थित ढंग है जिसके द्वारा कोई ……….अध्ययन किया जाता है।
उत्तर- वैज्ञानिक
v) जाति एक…….. वर्ग है।
उत्तर- बन्द
प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के चार सम्भावित उत्तर दिए गये हैं इनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखिए ।
(1) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए की गयी है।
i) 14 वर्ष
ii) 10 वर्ष
iii) 20 वर्ष
iv) 25 वर्ष
उत्तर- i) 14 वर्ष
( 2 ) "आत्महत्या" पुस्तक के लेखक थे -
i) कार्ल मार्क्स
ii) मैक्स वेबर
iii) इमाइल दुर्खीम
iv) जी. एस. धुरिये
उत्तर- iii) इमाइल दुर्खीम
( 3 ) महानगर कहा जाता है, जिनकी जनसंख्या -
i) 5 लाख
ii) 8 लाख
iii) 9 लाख
iv) 10 लाख से अधिक
उत्तर- iv) 10 लाख से अधिक
( 4 ) "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।" यह कथन है -
i) एम. डी. जॉनसन का
ii) अरस्तू का
iii) बोगार्डस का
iv) ऑगबर्न का
उत्तर- ii) अरस्तू का
Note For Important -
अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे आपको लिंक दी जा रही है उस पर क्लिक करके आप जिस सब्जेक्ट के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। उस पर क्लिक कर दीजिएगा।
(5) भारत में मुगल शासन काल में अल्पसंख्यक माना गया -
i) हिन्दुओं को
ii) मुसलमानों को
iii) ईसाईयों को
iv) अंग्रेजो को
उत्तर- ii) मुसलमानों को
प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए -
1. सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ?
उत्तर- एम.डी. जॉनसन
2. सांस्कृतिक विलम्बना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की ?
उत्तर- ऑगबर्न
3. नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति व्यवस्था आदि सामाजिक संरचना किस स्वरूप के तत्व है ?
उत्तर- संरचनात्मक
4. जब एक वर्ग पूरी तरह आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे क्या कहते हैं ?
उत्तर- जाति
5. मनुष्य जिन विभिन्न विश्वासों, प्रथाओं, परम्पराओं और शिष्टाचार के तरीकों में जीवन व्यतीत करता है उन सभी से किस संस्कृति का निर्माण होता है ?
उत्तर- अभौतिक
प्रश्न 4. सत्य असत्य लिखिए -
1. परिवार, नातेदारी - समूह जाति, रक्त संबंधी समूह है।
उत्तर- सत्य
2. किसी तथ्य को बातचीत के द्वारा समझने के स्थान पर स्वयं अपनी गहन दृष्टि से समझने की प्रक्रिया का नाम प्रश्नावली है।
उत्तर -असत्य
3. अवलोकन बहुत से प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से - संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते है।
उत्तर- असत्य
4.प्रकार्यात्मक पद्धति को समझने के लिए पहले कार्य शब्द के अर्थ को समझाना जरूरी है।
उत्तर- सत्य
5. शक्ति और अधिकारों के असमान सामाजिक विभाजन को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते है।
उत्तर- सत्य
प्रश्न. 5 जोड़ी बनाइए -
(1) जी एस. धुरये सन् 1894
(2) डी. पी. मुकर्जी 12 दिसम्बर, 1893
(3) राधाकमल मुकर्जी 26 दिसम्बर सन् 1887
(4) विनय कुमार सरकार सन् 1952
( 5 ) इण्डियन सोशियोलॉजिकल सोसायटी -7 दिसम्बर सन् 1889
उत्तर-
1- 12 दिसम्बर, 1893
2- सन् 1894
3- 7 दिसम्बर सन् 1889
4- 26 दिसम्बर सन् 1887
5- सन् 1952
प्रश्न 6. भारत में समाज शास्त्र के अध्ययन के कोई चार लाभ लिखिए।
उत्तर . समाजशास्त्र इतना महत्वपूर्ण विषय है यह पूरे सामाजिक जीवन को समझने में हमारी सहायता करता है। समाजशास्त्र ने सामाजिक ज्ञान के विकास और समाज को संगठित बनाने के क्षेत्र में जो योगदान किया है इसके लाभ निम्नलिखित है-
(1) मानव व्यवहारों का समुचित ज्ञान- समाजशास्त्र हमें उन नियमों से परिचित कराता है, जो हमारे सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं इन्हीं की सहायता से विभिन्न समूहों के आपसी विभेदों को कम करके सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
(2) सामाजिक समस्याओं को समझने में सहायक -
भारतीय समाज में आज अनेक गम्भीर समस्याएँ मौजूद है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, परिवारिक विघटन, अपराध नैतिकता का गिरता हुआ स्तर कुछ ऐसी समस्याएँ है उन समस्याओं का समाधान आर्थिक अथवा राजनीतिक आधार पर नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा ही इनके मूल कारणों को समझकर व्यावहारिक नीतियाँ बनाना सम्भव है।
(3) भावात्मक एकीकरण का आधार -
भावात्मक एकीकरण उन समाजों के लिए सबसे अधिक जरूरी है जिनमें एक दूसरे से अलग धर्मों संस्कृतियों, प्रजातियों, विश्वासों मनोवृत्तियों और रूचियों वाले लोग साथ-साथ रहते है। समाजशास्त्र अपने अध्ययनों के द्वारा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और प्रजातियों की एकता सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करता है इससे सभी समूहों को एक-दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है। समाज के प्रति एक तार्किक और निष्पक्ष दृष्टिकोण के द्वारा भी यह भावनात्मक एकीकरण को बढ़ाता है।
(4) पारिवारिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण -वर्तमान युग में हमारे जीवन की एक प्रमुख समस्या पारिवारिक जीवन में बढ़ते हुए तनाव और परिवारों का विघटन होना है सभी समाजों की तरह भारत में भी विवाह विच्छेद की बढ़ती हुई दर बच्चों के पालन-पोषण सम्बन्धी कठिनाइयों पति-पत्नी के बीच तनाव, परिवार में वृद्ध सदस्यों की उपेक्षा, युवा पीढ़ी की बढ़ती हुई निरंकुशता तथा पारिवारिक असुरक्षा आज पारिवारिक जीवन की प्रमुख समस्याएँ है।
अथवा
समाज शास्त्र के आराम्भिक विकास से संबंधित किन्ही चार समाज शास्त्रियों के नाम लिखिए।
प्रश्न 7. परिवार की परिभाषा दीजिए तथा परिवार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए ?
उत्तर .विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार को इसके आकार, ऐतिहासिकता तथा कार्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न रूप में परिभाषित किया है।
मैकाइवर तथा पेज के अनुसार -परिवार वह छोटा समूह है जो यौन-सम्बन्धों पर आश्रित है तथा सन्तान के जन्म और पालन-पोषण की व्यवस्था करता है।
परिवार की प्रमुख विशेषताएँ- मैकाइवर और पेज तथा किंग्सले डेविस ने परिवार की प्रकृति को अनेक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार है -
(1) सार्वभौमिकता -
सभी संस्थाओं और समितियों में परिवार सबसे अधिक सार्वभौमिक है। परिवार की सार्वभौमिकता का कारण यह है कि यह व्यक्ति की उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जिन्हें किसी भी दूसरे समूह द्वारा नहीं किया जा सकता।
(2) छोटा आकार - परिवार के सदस्य केवल वे व्यक्ति ही होते है जिन्होंने इसमें जन्म लिया हो अथवा विवाह सम्बन्ध स्थापित किये हैं।
(3) सदस्यों का असीमित दायित्व -
परिवार में किसी भी सदस्य के दायित्वों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती इसमें व्यक्ति सभी कार्य करता है जो दूसरे सभी सदस्यों के लिए उपयोगी होता हैं।
(4) परम्पराओं की प्रधानता -
परिवार एक ऐसा समूह है जो अनेक सांस्कृतिक और परम्परागत नियमों पर आधारित होता है।
(5) रचनात्मक प्रभाव
परिवार में सभी सदस्य अपने व्यवहारों के द्वारा एक दूसरे को रचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं तथा पारस्परिक सहयोग को बढ़ाते है -
( 6 ) भावनात्मक आधार
( 7 ) सामाजिक ढाँचे में केन्द्रीय स्थिति
(8) परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति
अथवा
विवाह की परिभाषा दीजिए तथा विवाह के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए ?
प्रश्न 8. संस्कृति के अर्थ तथा प्रकारों की विवेचना कीजिए।
उत्तर- अर्थ – संस्कृति उन अनेक भौतिक तथा बौद्धिक साधनों की सम्पूर्णता है जिनके - द्वारा मानव अपनी जैविकीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करके अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। अर्थात मुनष्य द्वारा सीखे हुए सभी व्यवहारों की सम्पूर्णता संस्कृति कहलाती है। संस्कृति का प्रकार संस्कृतियों को विद्वानों ने चार भागों में विभाजित किया है-
(1) आध्यात्मिक संस्कृति
(2) भौतिकवादी संस्कृति
(3) सुखवादी संस्कृति
(4) आक्रामक संस्कृति
संस्कृति एक परिवर्तनशील तथ्य है। मनुष्य के अनुभवों तथा जरूरतों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। सभी समाजों की सांस्कृतिक विशेषताएँ एक-दूसरे से कुछ अलग होती है। इस आधार पर विद्वानों ने संस्कृतियों के अनेक रूपों का उल्लेख किया है। इनमें आध्यात्मिक संस्कृति, भौतिकवादी संस्कृति, सुखवादी संस्कृति तथा आक्रामक संस्कृति कुछ प्रमुख रूप है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता अधिक दिखाई देती है। इसी कारण यहाँ प्रति-संस्कृति की दशा भी प्रभावी बनी है।
अथवा
संस्कृति तथा पर्यावरण के संबंध को समझाइए ।
प्रश्न 9. प्रतिस्पर्द्धा के मुख्य प्रकारों को संक्षेप में समझाइए।
उत्तर.मर्सर और वाडर ने अपनी पुस्तक "द स्टडी ऑफ सोसाइटी में प्रतिस्पर्द्धा के चार मुख्य रूपों का उल्लेख किया है।
(1) विशुद्ध तथा सीमित प्रतिस्पर्द्धा -
जब दो पक्षों के बीच बिना किसी सांस्कृतिक या आर्थिक नियमों के स्वतन्त्र रूप से प्रतिस्पर्द्धा होती है तो इसे विशुद्ध प्रतिस्पर्द्धा कहा जाता है। जबकि सीमित प्रतिस्पर्द्धा वह है जो कुछ नियमों को ध्यान में रखकर की जाती है।
(2) निरपेक्ष और सापेक्ष प्रतिस्पर्द्धा -
जब किसी एक पद को पाने के लिए अनेक लोग एक-दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करते है, तब इसे निरपेक्ष प्रतिस्पर्द्धा कहा जाता है। जबकि सापेक्ष प्रतिस्पर्द्धा वह है, जो बहुत से लोगों द्वारा समाज में विशेष प्रतिष्ठा, संपत्ति या अधिकार पाने के लिये की जाती है।
(3) वैयक्तिक और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्द्धा -
जब प्रतिस्पर्द्धा ऐसे व्यक्तियों के बीच होती है। जो एक-दूसरे को वैयक्तिक रूप से जानते हुए उनके साथ अन्तर्क्रिया करने के बाद भी उनसे आगे निकलने का प्रयास करते है, तब इसे वैयक्तिक प्रतिस्पर्द्धा कहते है। जबकि अवैयक्तिक प्रतिस्पर्द्धा वह है जिसमें हम उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते जिनसे हम प्रतिस्पर्द्धा कर रहे होते है।
(4) रचनात्मक तथा हानिकारक प्रतिस्पर्द्धा-
रचनात्मक प्रतिस्पद्धा वह है जो समाज के लिए लाभप्रद होती है। जबकि हानिकारक प्रतिस्पर्द्धा में कुछ लोग तात्कालिक लाभ पाने के लिये समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों का सहारा लेने लगते है ।
अथवा
संघर्ष की किन्हीं चार विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
प्रश्न 10. जनसंख्या वृद्धि किस तरह सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देती है। -
उत्तर . बहुत-से विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण समाज की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं में परिवर्तन होना माना है इनका विचार है कि समाज की विभिन्न संस्थाओं, नियमों और परम्पराओं का विकास उसकी जनसंख्या के आकार के अनुसार ही होता है। जनसंख्या कम होने पर परम्परागत जीवन को प्रोत्साहन मिलता है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन की जरूरत महसूस की जाने लगती है। इसी प्रकार जनसंख्या की विशेषताओं में होने वाला परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है।
उदाहरण -
जब किसी समाज की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के अनुपात में अधिक अन्तर हो जाता है, तब सामाजिक सन्तुलन बिगड़ने लगता है। इससे व्यवहार के तरीकों में भी परिवर्तन होता है।
इसी तरह जनसंख्या में यदि वृद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है तो परम्पराओं का प्रभाव बढ़ता है, जबकि युवा वर्ग की संख्या अधिक होने से सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा मिलती है। सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारकों के प्रभाव को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में स्वतंत्रता के समय देश की जनसंख्या जहाँ 33 करोड़ थी, वही सन् 2007 तक यह लगभग 117 करोड़ हो गयी। इसके फलस्वरूप परिवार नियोजन के व्यापक कार्यक्रम के साथ ही शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन हुआ। संयुक्त परिवारों की जगह एकाकी परिवारों को प्रोत्साहन मिला। नगरी करण में वृद्धि हुई तथा व्यक्तियों के सम्बन्धों की प्रवृत्ति बहुत अधिक बदल गयी।
अथवा
क्रान्ति और प्रगति में क्या अन्तर है ?
प्रश्न 11. पर्यावरण के अर्थ को समझाइए ?
उत्तर . शाब्दिक रूप से पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है-परि+आवरण / परि' का अर्थ है 'चारों ओर' तथा 'आवरण' का अर्थ है 'ढके हुए। इससे स्पष्ट होता है। कि पर्यावरण का आशय उन सभी दशाओं से है जो किसी प्राणी या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है। पर्यावरण के अनुसार ही विभिन्न समुदायों की संरचना एक विशेष तरह से बनती और विकसित होती है। पर्यावरण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए लेण्डिस ने इसके तीन प्रमुख भागों को स्पष्ट किया है. -
1. प्राकृतिक पर्यावरण- वे सभी प्राकृतिक शक्तियाँ जिनकों मनुष्य प्रभावित नही कर - सका है, प्राकृतिक पर्यावरण के अन्तर्गत आती है।
उदाहरण जलवायु, तापमान, ऋतुएँ, भूमि की बनावट, खनिज पदार्थ, वर्षा, तरह-तरह की वनस्पतियाँ तथा ग्रहों और नक्षत्रों का परिचलन आदि हमारा प्राकृतिक
पर्यावरण है। इसी को हम भौगोलिक पर्यावरण भी कहते है। उदाहरणार्थ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भूकंप संभावित क्षेत्र अथवा बर्फीले क्षेत्र अथवा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों की बनावट भिन्न-भिन्न होती है।
2. सामाजिक पर्यावरण- जो दशाएँ हमारे सामाजिक जीवन का निर्माण करती है, वे - व्यक्ति का सामाजिक पर्यावरण होती है । किसी समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्ग, सामाजिक संगठन, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, समाज के मूल्य आदि सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
3. सांस्कृतिक पर्यावरण -मनुष्य ने अपने प्रयासों, बुद्धि और अनुभव के द्वारा जितने भी भौतिक और अभौतिक आविष्कार किये है, वे सभी व्यक्ति और समाज के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करते है।
उदा०- उत्पादन के तरीके, भौतिक आविष्कार, रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास, कला, भाषा, कानून, फैशन के तरीके उपकरण तथा संचार के साधन आदि सामाजिक व्यवस्था को विकसित करते हैं, इनकी सम्पूर्णता को ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की सम्पूर्णता को ही सम्पूर्ण पर्यावरण कहा जाता है।
अथवा
पर्यावरण के आधार पर गाँव और नगर की तुलना कीजिए?
प्रश्न 12. पूँजीवादी व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?
उत्तर . पूँजीवादी व्यवस्था की दो विशेषताएँ है -
(1) निजी सम्पत्ति की धारणा
( 2 ) लाभ की प्रवृति
समाज में व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त वस्तु के द्वारा ही अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते है। इसके फलस्वरूप सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले साधन और सुविधाएँ बहुत कुछ समान थी इसलिए आदिम समाज में न तो वर्ग विभाजन था और न ही किसी तरह का वर्ग संघर्ष पाया जाता था। इसके बाद जब उत्पादन प्रणाली पर कुछ लोगों का एकाधिक शुरू हुआ और निजी सम्पत्ति की धारणा को प्रोत्साहन मिला तब समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित होने लगा। विभिन्न युगों में यह वर्ग मालिक और दास सामंत और अर्थ दास किसान कुलीन लोग और साधारण जनता, पूँजीपति और श्रमिक के रूप में सामने आऐ । विभिन्न युगों में इन मालिकी सामान्तों कुलीन लोगों और पूँजीपतियों ने उत्पादन का कार्य उस वर्ग के द्वारा किया जाता रहा। जिसका उत्पादन के साधनों पर किसी तरह का अधिकार नहीं होता था। इससे स्पष्ट होता है जब कोई शोषित वर्ग का असन्तोष लगातार बढ़ता जाता हैं तो इसी सन्तोष से वर्ग संघर्ष का जन्म होता है।
अथवा
पूँजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है ? -
प्रश्न 13. समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर. राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य की उत्पत्ति राज्य व्यवस्था और शासन के सिद्धान्तों की विवेचना करता है इन दोनों विज्ञानों का सम्बंध अनेक तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। सर्व प्रथम इन दोनों विज्ञानों का उद्देश्य व्यक्ति का समाजीकरण करना तथा एक नियमबद्ध जीवन का प्रशिक्षण देना है दूसरे समाज शास्त्र के द्वारा जिन नियमों की खोज की जाती है उन्हीं की सहायता से राज्य को अधिक संगठित बनाना सम्भव हो पाता है तीसरे वर्तमान रूप में राज्य को कानूनों द्वारा सामाजिक जीवन को संगठित बनाना सम्भव हो सकता है। चौथे अनेक विषयों जैसे कानून परम्परा, - जनमत, नेतृत्व सामाजिक नियंत्रण तथा राजनीतिक दल आदि का अध्ययन समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में समान रूप से किया जाता है यही कारण है कि दोनों विज्ञान एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बंध है।
अथवा
समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं ?
प्रश्न 14. आर्थिक संस्थाएँ किस तरह अर्थव्यवस्था के रूप का निर्धारण करती हैं ?
उत्तर.आर्थिक संस्था का आशय उन सभी नियमों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं को नियमित किया जाता है जब अनेक आर्थिक संस्थाएं मिलकर एक विशेष आर्थिक तन्त्र का निर्माण करती हैं, तब इसे हम अर्थव्यवस्था कहते है।
आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित बनाने वाली संस्थाओं में कुछ संस्थाएँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह है (1) सम्पत्ति (2) श्रम विभाजन (3) संविदा, (4) बाजार, (5) विनिमय प्रणाली, (6) प्रतियोगिता, (7) आधुनकि व्यवसाय इन संस्थाओं की प्रकृति के अनुसार जिन आर्थिक संबंधों का विकास होता है, उन्हीं से एक विशेष तरह की अर्थव्यवस्था विकसित होती है।
दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है- (1) आदिम अर्थ व्यवस्था, (2) कृषि अर्थ व्यवस्था तथा (3) औद्योगिक अर्थ व्यवस्था आदिम अर्थ व्यवस्था सरल समाजों की वह विशेषता है जिसमें सभी आर्थिक संस्थाओं का रूप बहुत सरल होता है। कृषि अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित होती है तथा इसमें आर्थिक परिवर्तन नहीं होता। औद्योगिक अर्थ व्यवस्था औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम है जो आज दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद है।
अथवा
सरकार से आप क्या समझते हैं ? सरकार के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए
प्रश्न 15. समाजीकरण के मुख्य सिद्धान्तों की संक्षेप में विवेचना कीजिए ।
उत्तर. समाजीकरण के सिद्धान्त समाजीकरण के उद्देश्यों तथा प्रक्रिया को विभिन्न विद्वानों ने अनेक सिद्धान्तों के रूप में स्पष्ट किया है। एक ओर चार्ल्स कूले मीड तथा फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक आधार पर "आत्म" के विकास को समाजीकरण का उद्देश्य बताया है जबकि दुर्खीम ने सामाजिक संरचना तथा सामूहिक चेतना के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। वास्तव में विभिन्न समाजों में समाजीकरण की प्रक्रिया का रूप एक विशेष समाज की जरूरतों, परिस्थितियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होता है।
अथवा
व्यक्तित्व-निर्माण के सांस्कृतिक कारक कौन से हैं ?
प्रश्न 16. सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए ।
उत्तर .सामाजिक संरचना की परिभाषाएं-
1. गिन्सबर्ग - गिन्सबर्ग के शब्दों में सामाजिक संरचना का सम्बन्ध सामाजिक संगठन के प्रमुख है ।" स्वरूपों अर्थात विभिन्न समूहों, समितियों तथा संस्थाओं आदि के संकुल से
2. कोजर - कोजर ने लिखा है कि "सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित सम्बन्धों से है।"
सामाजिक संरचना की विशेषताएँ - सामाजिक संरचना की अवधारणा को इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के आधार पर निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है :-
1. सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता है- जिन इकाइयों के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, वे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होती है। यही क्रमबद्धता सामाजिक संरचना के विशेष स्वरूप को स्पष्ट करती है।
2. सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है सामाजिक संरचना का निर्माण- जिन समूहों तथा संघों से होता है, उनकी प्रकृति अधिक स्थायी होती है। उदाहरण के लिए समुदाय एक बड़ा समूह है, जबकि अनेक आर्थिक राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समितियाँ छोटे समूह हैं। छोटे समूहों और उनके सदस्यों की प्रकृति में परिवर्तन होने पर भी समुदाय की संरचना में साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं होता।
3. सामाजिक संरचना की अनेक उप संरचनाएँ होती है- सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों की संरचना को उनकी उप-संरचना कहा जाता है जैसे राज्य सरकार राजनैतिक दल तथा दाबाव समूह एक राजनैतिक संरचना की उप-संरचनाएँ हैं।
4. सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग आपस में सम्बन्धित होते है - सामाजिक संरचना की उप-संरचनाएँ एक-दूसरे से सम्बन्धित रहकर किसी सामाजिक संरचना को उपयोगी और प्रभावशाली बनाती है।
5. - सामाजिक संरचना में अनेक मूल्य शामिल होते है - व्यवहार और सम्मान के अनेक तरीके, जनरीतियाँ, प्रभाएँ, परम्पराएँ तथा इस बात का निर्धारण करते है कि किसी सामाजिक संस्थान की प्रकृति किस प्रकार की होगी। इनके आधार पर ही परम्परागत संरचना अथवा वर्गों पर आधारित सामाजिक संरचना का निर्माण होता है।
6. सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के निर्धारित प्रकार्य होते है- इन प्रकार्यों का निर्धारण सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा होता है। इसी कारण लोगों का यह प्रयत्न रहता है कि अपनी सामाजिक संरचना के मूल्यों में कोई परिवर्तन न होने दे।
अथवा
नृजातिकी के अर्थ तथा स्तरीकरण से इसके संबंध की विवेचना कीजिए ।
प्रश्न 17. सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है ? इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए ।
उत्तर. सामाजिक पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी समुदाय पर भौतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दशाओं के प्रभाव का अध्ययन करता है। "समाजशास्त्र के अन्तर्गत सामाजिक पारिस्थितिकी विभिन्न समुदायों तथा उनके पर्यावरण के सम्बन्ध का अध्ययन है।" परिभाषा - (ऑगबर्न निमकॉफ के अनुसार ) "मानव पारिस्थितिकी मानव प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के आपसी संबंध को स्पष्ट करती है।"
सामाजिक पारिस्थितिकी के तत्व -
मेकेन्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के तत्वों को चार मुख्य भागों में विभाजित किया है -
1. पर्यावरण - सामाजिक पारिस्थितिकी का पहला तत्व पर्यावरण है इसका सम्बन्ध उन सभी भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्वों से है जो समुदाय की संरचना तथा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करते है। उदाहरण के लिए, जलवायु, तापक्रम, खनिज पदार्थ, भूमि की बनावट भूमि का उपजाऊपन, समुद्र तथा नदियाँ अदि भौगोलिक तत्व है। दूसरी ओर धार्मिक नियम, विश्वास, प्रथाएँ, परम्पराएँ तथा व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुऐं सांस्कृतिक तत्व है।
2. जनसंख्या - सामाजिक के निर्माण में जनसंख्या की विशेषताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत जनसंख्या का आकार जनसंख्या का धनत्व, स्वास्थ्य, सम्बन्धी विशेषताएं जन्म दर तथा मृत्य दर जनसंख्या में समरूपता अथवा विभिन्नता आदि मुख्य तत्व है।
3. वसाहट का स्वरूप - वसाहट या अधिवास के स्वरूप का आशय केवल मकानों की बनावट से ही नहीं है बल्कि रहने के स्थान के चारों और की परिस्थितियों, रहन-सहन का ढंग तथा जीवन स्तर का भी मानव वसाहट से महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है।
4. अर्थ व्यवस्था - मानव की परिस्थितिकी में आर्थिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। कोई समुदाय जीवन-यापन के लिए पशुओं के शिकार पर निर्भर होता है, कहीं खेती के द्वारा जीविका उपर्जित की जाती है, कोई समुदाय दस्तकारी पर निर्भर होता है, जबकि किसी समुदाय में विकसित श्रम विभाजन और विशेषीकरण के द्वारा आर्थिक क्रियाएँ की जाती है ।
5. सामाजिक संगठन - परिवार का संगठन, नातेदारों की प्रवृत्ति आदि ।
6. प्रौद्योगिकी - ज्ञान तथा उपकरण जिनके द्वारा व्यक्ति भौगोलिक दशाओं पर नियन्त्रण स्थापित करके अपनी जरूरतों को पूरा करता है।
अथवा
औद्योगिक नगर तथा महानगर के अर्थ और विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
प्रश्न 18. समाजशास्त्र के लिए मैक्स वेबर के योगदान की संक्षेप में विवेचना कीजिए।
उत्तर . वेबर ने ऐतिहासिक सम्प्रदाय के इस विचार को नहीं माना कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। वेबर के अनुसार यदि हम सभी तरह के सामाजिक घटनाओं का अध्ययन न करे बल्कि कुछ अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं का ही अध्ययन करें जिससे वैज्ञानिक मानदण्ड को बनाये जा सके। यह महत्वपूर्ण घटनाये कौन-कौन सी है; इसे उन्होंने समाजशास्त्र को नये सिरे से परिभाषित करके स्पष्ट किया। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक बोध करने का इस तरह प्रयास करता है जिससे उसके कारणों तथा परिणामों को समझा जा सके। इस परिभाषा के द्वारा वेबर ने यह स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया है। दूसरी ओर सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति की उपयोग कर सकते है वह व्याख्यात्मक बोध की प्रणाली है।
1. सामाजिक क्रिया - वेबर के अनुसार क्रिया तथा व्यवहार एक-दूसरे से अलग धारणाएँ है। वास्तव में व्यवहार का क्षेत्र क्रिया तुलना में कही अधिक व्यापक है क्योंकि इसके अन्तर्गत वे व्यवहार भी आ जाते है जो मुनष्य की इक्छा, बुद्धि अथवा दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होते। दूसरी ओर क्रिया का सम्बन्ध मनुष्य के केवल उन्हीं व्यवहारो से है जो अर्थ पूर्ण होते है। अर्थात जिन कार्यो को करने में कर्ता की प्रेरणाओं पर दूसरे
व्यक्तियों के दृष्टिकोण और क्रियाओं का प्रभाव पड़ा हो तथा जो कार्य अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर रहे हों, उन्हीं को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है।
2. व्याख्यात्मक बोध -सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किस ढगं से किया जाय ? - इसके लिए वेबर ने जिस प्रणाली को प्रस्तुत किया उसे व्याख्यात्मक बोध कहा जाता है। व्याख्यात्मक बोध का आशय एक विशेष घटना को तर्कपूर्ण ढंग समझना है ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब व्यक्ति भवना में बहकर कोई निर्णय न ले। इस प्रकार व्याख्यात्मक बोध एक ऐसी प्रणाली है जो भावनात्मक निर्णय से दूर रहकर तर्कपूर्ण ढंग से घटनाओं का अध्ययन करने और कारणों की खोज करने पर जोर देती है।
3. आदर्श प्रारूप -वेबर ने आदर्श प्रारूप को ऐसे साधन के रूप में स्पष्ट किया जिसके - द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्याख्यात्मक बोध किया जा सकता है। आदर्श प्रारूप के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वेबर ने बताया कि समान विशेषताओं वाली घटनाओं से जब मुख्य सैद्धांतिक श्रेणी का निर्माण होता है तो उसी को आदर्श प्रारूप कहते हैं।
(1) आदर्श प्रारूप का सम्बन्ध समाज में घटित होने वाली केवल महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करने से है।
(2) आदर्श प्रारूप की प्रकृति इसलिए सामाजिक होती है कि इन्हें पूरे समाज की स्वीकृति मिली होती है।
(3)आदर्श प्रारूप की प्रकृति हमेशा एक सी नहीं रहती बल्कि इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।
(4) इसके अन्तर्गत प्रत्येक क्रिया को उसी अर्थ में समझा जाता है।
अथवा
समाजशास्त्र के लिए दुर्खीम के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
प्रश्न 19. धुरये के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताएँ क्या हैं ?
उत्तर. धुरये ने जाति व्यवस्था संरचना और इससे सम्बन्धित नियमों को स्पष्ट करने के लिए जाति की अग्र छः विशेषताओं का उल्लेख किया -
(1) जाति व्यवस्था एक-दूसरे से भिन्न प्रस्थितियों और भूमिकाओं वाले अनेक समूहों या खण्डों में विभाजित होती है।
(2) जाति व्यवस्था के सभी खण्डों की सामाजिक स्थिति के बीच एक निश्चित संस्तरण होता है जिसमें ब्राह्मणों की प्रस्थित सर्वोच्च है।
(3) विभिन्न जातियों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी ही जाति में भोजन और सामाजिक सम्पर्क के सम्बन्ध स्थापित करें।
(4) जातियों की उच्चता और निम्नता के अनुसार ही उनकी नियोग्यताओं और विशेषाधिकारों का निर्धारण होता है।
(5) प्रत्येक जाति का अपना अनुवंशिक व्यवसाय होता है।
(6) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में विवाह करना आवश्यक है।
अथवा
परम्परा के बारे में डी. पी. मुकर्जी के विचार क्या हैं ?
प्रश्न 20. प्राथमिक समूह से आप क्या समझते है ? प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर . कूले ने लिखा है कि "प्राथमिक समूहों से मेरा अभिप्राय उन समूहों से है जिनकी मुख्य विशेषता आपने-सामने से घनिष्ठ सम्बन्ध और सहयोग की भावना है। यह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और मनोवृत्तियों का निर्माण करने में प्राथमिक होते हैं। 'इस प्रकार छोटा आकार सदस्यों के बीच शारीरिक समीपना, सम्बन्धों में स्थायित्व, सदस्यों के लक्ष्यों में समानता और प्राथमिक नियन्त्रण इन समूहों की प्रमुख विशेषताएँ है।
कूले के अनुसार द्वितीयक समूह वे हैं जिनकी विशेषताएँ प्राथमिक समूहों से भिन्न होती हैं। प्राथमिक तथा द्वितीय समूहों के बीच निम्नांकित अन्तर अधिक महत्वपूर्ण है-
(1) प्राथमिक समूह आकार में बहुत छोटे होते हैं। द्वितीयक समूहों का आकार बड़ा होता हैं।
(2) प्राथमिक समूहों के सदस्यों के बीच शारीरिक समीपता होती है। द्वितीयक समूहों के सदस्यों के सम्बन्ध अप्रत्यक्ष होते हैं।
(3) प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य होती हैं जबकि द्वितीयक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती हैं।
(4) प्राथमिक समूहों में व्यक्तियों के सम्बन्ध वैयक्तिक होते हैं तथा उनके लक्ष्यों एवं मनोवृत्तियों में समानता होती हैं। द्वितीयक समूहों में सम्बन्ध औपचारिक होने के अतिरिक्त उनके स्वार्थ एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।
(5) अनौपचारिक नियन्त्रण प्राथमिक समूहों की विशेषता हैं। द्वितीयक समूहों में नियन्त्रण का रूप औपचारिक होता है।
(6) प्राथमिक समूह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं तथा सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाना है। दूसरी ओर द्वितीयक समूह व्यक्तित्व के रूप में छोटे से हिस्से को ही प्रभावित करते हैं तथा सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष सहयोग होना है।
(7) प्राथमिक समूहों का विकास स्वाभाविक रूप से होना है जबकि द्वितीयक समूह योजना बद्ध रूप से संगठित किये जाते है।
अथवा
संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक जीवन में संस्कृति की भूमिका को समझाइए ।
प्रश्न 21. प्रश्नावली के प्रमुख प्रकार कौन से है ? विवेचना कीजिए ।
उत्तर. प्रश्नावली तथ्यों को संकलित करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह बहुत से प्रश्नों की एक सूची है, जिन्हें उत्तर देने के लिए संबंधित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दिया जाता है। गुँदे तथा हार के शब्दों में साधारण तथा प्रश्नावली का आशय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की एक ऐसी विधि से है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र को भरकर विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ भेजता है।
प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की सूची है। इसमें अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों में सम्बंधित प्रश्नों का समावेश होता है। प्रश्नावली के चार प्रकार मुख्य है बन्द - प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रपूर्ण प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली
1. बन्द प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे कुछ उत्तर दिए रहते हैं। उत्तरदाता को इन्हीं में से किसी एक उत्तर को चुनना होता है।
2. खुली प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे कोई उत्तर नहीं होता उत्तर दाता अपनी इच्छा से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है।
3. चित्रपूर्ण प्रश्नावली में प्रश्न के आगे उत्तरों की जग कुछ चित्र बने होते हैं। इन चित्रों को देखकर अशिक्षित व्यक्ति भी अपनी पसन्द के उत्तर का चुनाव कर सकते है।
4.मिश्रित प्रश्नावाली में कुछ प्रश्न खुले हुए होते हैं तो कुछ बन्द प्रकृति के होते हैं। आवश्यकतानुसार इसमें प्रश्न के आगे कुछ चित्रों का भी उपयोग किया जा सकता है।
अथवा
अवलोकन के मुख्य प्रकार क्या हैं? विवेचना कीजिए ।
इसे भी पढ़ें 👇👇👇👇
MP Board class 11th Hindi varshik paper solution 2023
MP Board class 11th Biology varshik paper 2023
MP Board class 11th business studies varshik real paper 2023
MP Board class 11th History varshik paper 2023
MP Board class 11th economics varshik paper 2023
MP Board class 11th sociology varshik paper 2023
MP Board class 11th Geography varshik paper 2023
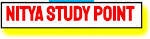

Post a Comment